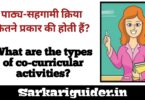रुचि की विशेषताएँ (Characteristics of Interest)
रुचि की विशेषताएँ- परामर्श एवं निर्देशन कार्य के लिए रुचियाँ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण हैं। ये अधिगम एवं कक्षा को महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बनाती हैं। रुचि की विशिष्ट विशेषताओं वर्णन निम्नलिखित है-
(1) रुचि व्यक्तित्व का एक अंग है। सम्पूर्ण मानस व्यवहार का एक पहलू है।
(2) रुचि अनुभव में संलग्नता की प्रवृत्ति है।
(3) रुचि वंशानुक्रम एवं वातावरण से प्रभावित होती है।
(4) आयु बढ़ने के साथ-साथ रुचियों की विभिन्नता समाप्त हो जाती है।
(5) रुचि किसी क्रिया के प्रति आकर्षित होने, पसन्द करने एवं सन्तुष्टि पाने प्रवृत्ति है।
(6) रुचि सुखान्त भावनाओं या व्यवहार के आकर्षण का प्रतिबिम्ब है।
(7) रुचि किसी वस्तु के प्रति जाग्रत होने, प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति है।
(8) रुचि किसी वस्तु के प्रति ध्यान केन्द्रित करने वाली प्रवृत्ति है, रुचि एवं एक ही सिक्के के दो पहलू है।
(9) रुचि व्यवहार के समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है।
रुचियों के स्रोत (Sources of Interest)-
रुचि के क्षेत्र में हुए विभिन्न अनुसन्धानों के परिणामों के आधार पर स्वीकारा जाता है कि पियों का जन्म मनो-शारीरिक कारणों से होताना इसके विकास में अन्य मनोवैज्ञानिक पहलुओं की भाँति वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतः कहा जा सकता है कि रुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है।
सुपर के अनुसार- “रुचि की उत्पत्ति में जहाँ एक ओर जन्मजात अधिक्षमता एवं अन्तःस्रावी तत्व सहायक होते हैं, वहाँ दूसरी ओर सुविधाओं एवं सामाजिक मूल्यांकन का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ वस्तुएँ जिन्हें व्यक्ति भली-भाँति चाहता है तथा जो उसको मान्यता एवं सन्तुष्टी प्रदान करती है रुचि कहलाती है। यही नहीं, कुछ व्यक्तियों के किसी कार्य को करने की रुचि अपने साथियों के तादात्म्य से होती है। कभी-कभी व्यक्ति स्वयं भी रुचि के प्रति अपना प्रत्यय बना लेता है।
उक्त विचार के विपरीत रुचि के सम्बन्ध में दूसरी आधुनिकतम विचारधारा यह है कि जन्मजात न होकर अर्जित होती है। आदत एवं क्षमताओं की तरह इनको भी समाज रटकर,. समाज के साथ अन्तःक्रिया करके अर्जित किया जाता है। समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का इनके विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। थोर्नडाइक का इस सम्बन्ध में निष्कर्ष है कि ‘रुचि अर्जित की जाती है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि विकास में विभिन्न तथ्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इच्छाएँ, आवश्यकताएँ, अभाव, अनुभव, सुविधाएँ, संस्कृति शिक्षा आदि ऐसे तत्व हैं जो रुचियों के निर्धारण के आधार है। इन तथ्यों के परिवर्तन से रुचियों के परिवर्तन परिलक्षित होता है। अतः कह सकते हैं कि रुचियों में गत्यात्मकता पाई जाती है। समाज की परिस्थितियों, सुविधाओं, स्वीकृतियों, मान्यताओं आदि के परिवर्तन से व्यक्ति की रुचियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। कुल मिलाकर रुचियाँ स्वरूप से परिवर्तनशील होती हैं।
- बुद्धि का अर्थ और परिभाषा | Meaning and Definition of Intelligence in Hindi
- बुद्धि के प्रमुख सिद्धान्त|Theories of Intelligence in Hindi
- बुद्धि परीक्षण – बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, गुण, दोष, उपयोगिता – Buddhi Parikshan
- बुद्धि-लब्धि – बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि का मापन – Buddhi Labdhi
इसे भी पढ़े ….
- निर्देशात्मक परामर्श- मूलभूत अवधारणाएँ, सोपान, विशेषताएं, गुण व दोष
- परामर्श के विविध तरीकों पर प्रकाश डालिए | Various methods of counseling in Hindi
- परामर्श के विविध स्तर | Different Levels of Counseling in Hindi
- परामर्श के लक्ष्य या उद्देश्य का विस्तार में वर्णन कीजिए।
- परामर्श का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति | Meaning, Definition and Nature of Counselling in Hindi
- विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
- विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन के क्षेत्र का विस्तार में वर्णन कीजिए।
- विद्यालय में निर्देशन प्रक्रिया एवं कार्यक्रम संगठन का विश्लेषण कीजिए।
- परामर्श और निर्देशन में अंतर
- विद्यालय निर्देशन सेवाओं के संगठन के आधार अथवा मूल तत्त्व
- निर्देशन प्रोग्राम | निर्देशन कार्य-विधि या विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन
- विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
- निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, तथा प्रकृति
- विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के लिए सूचनाओं के प्रकार बताइए|
- वर्तमान भारत में निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।
- निर्देशन का क्षेत्र और आवश्यकता
- शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन का महत्व
- व्यक्तिगत निर्देशन (Personal Guidance) क्या हैं?
- व्यावसायिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक निर्देशन की परिभाषा दीजिए।
- वृत्तिक सम्मेलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी क्रिया विधि का वर्णन कीजिए।
- व्यावसायिक निर्देशन की आवश्कता | Needs of Vocational Guidance in Education
- शैक्षिक निर्देशन के स्तर | Different Levels of Educational Guidance in Hindi
- शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य एवं आवश्यकता |
- शैक्षिक निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा | क्षेत्र के आधार पर निर्देशन के प्रकार
- शिक्षण की विधियाँ – Methods of Teaching in Hindi
- शिक्षण प्रतिमान क्या है ? What is The Teaching Model in Hindi ?
- निरीक्षित अध्ययन विधि | Supervised Study Method in Hindi
- स्रोत विधि क्या है ? स्रोत विधि के गुण तथा दोष अथवा सीमाएँ
- समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि /समाजमिति विधि | Socialized Recitation Method in Hindi
- योजना विधि अथवा प्रोजेक्ट विधि | Project Method in Hindi
- व्याख्यान विधि अथवा भाषण विधि | Lecture Method of Teaching