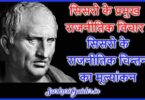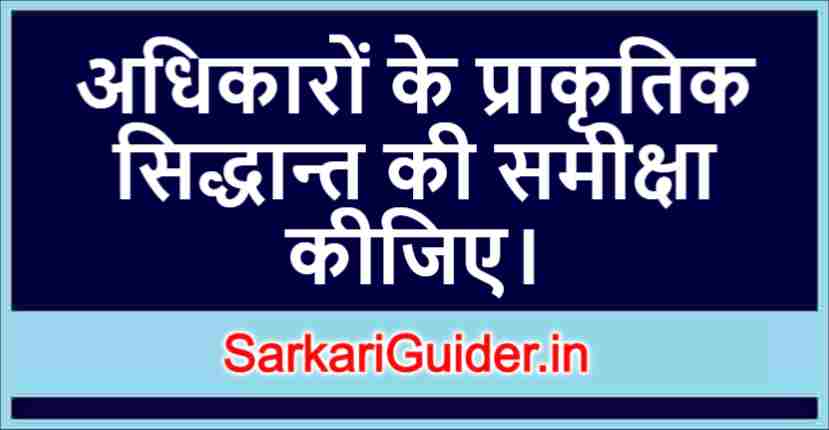
अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धान्त
अधिकारों के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त सबसे अधिक प्राचीन है, और इसका प्रचलन यूनानियों के समय से है। इस सिद्धान्त के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतया प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। इस सिद्धान्त के मतानुसार जैसा कि आशीर्वादम ने कहा है, “अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं। जिस प्रकार उसकी चमड़ी का रंग। इनकी विस्तृत व्याख्या करने या औचित्य बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तो स्वयंसिद्ध हैं।”
इस सिद्धान्त के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष और स्वयंसिद्ध हैं। वे व्यक्ति को प्रकृति की देन हैं और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए।
हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वाल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेन्सर, ब्लेकस्टोन, आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त का पोषण किया। सामाजिक समझौता सिद्धान्त के प्रतिपादक इस सिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। उनका अनुमान है कि प्रारम्भ से ही व्यक्ति के इस प्राकृतिक अधिकार थे और संविदा करते समय वह अपने इन अधिकारों में से कुछ को अपने से उच्च सत्ता को केवल इसलिए सौंप देता है कि उसके शेष अधिकारों की रक्षा हो सके। स्पेन्सर का विचार है कि समान स्वाधीनता का अधिकार सभी व्यक्तियों का मौलिक अधिकार हैं। लॉक के शब्दों में, “सभी मनुष्य स्वतन्त्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने के पूर्व ही व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। “
सिद्धान्त का प्रभाव – इस सिद्धान्त ने फ्रांस और अमरीका की क्रान्ति के प्रेरक सिद्धान्त के रूप में कार्य किया था और इसके आधार पर ही स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गयी थी। इस सिद्धान्त के आधार पर ही वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है।
आलोचना— अधिकारों के इस प्राकृतिक सिद्धान्त ने उस समय व्यक्ति के जीवन का मूल्य और महत्त्व स्थापित किया, जबकि मानव का महत्त्व पशुओं से अधिक नहीं समझा जाता था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में इस सिद्धान्त का अधिक महत्त्व नहीं है और निम्नलिखित आधारों पर इस सिद्धान्त की आलोचना की जा सकती है
(1) प्राकृतिक शब्द अस्पष्ट और भ्रामक – प्राकृतिक सिद्धान्त में जिस प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह पूर्णतया अनिश्चित है और अनेकार्थक है। प्रो. रिची के अनुसार, “प्राकृतिक शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, सृष्टि का वह भाग जहाँ मनुष्य नहीं है, आदर्श या पूर्ण, लक्ष्य, अपूर्व, साधारण या औसत। “
उपर्युक्त सिद्धान्त में प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः इस सिद्धान्त के किसी भी प्रतिपादन ने प्राकृतिक शब्द को स्पष्ट नहीं किया है। प्राकृतिक शब्द का अर्थ अनिश्चित होने के कारण यह सिद्धान्त भी नितान्त अनिश्चित एवं भ्रमपूर्ण हो जाता है।
(2) प्रतिपादक प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर एकमत नहीं – प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त थे अथवा वर्तमान समय में इस धारणा के अनुसार नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होने चाहिए, इस सम्बन्ध में सिद्धान्त एकमत नहीं हैं और इस एकमतता के अभाव में प्राकृतिक अधिकारों की कोई सूची नहीं बनाई जा सकती है। इस सिद्धान्त के कुछ समर्थक व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्राकृतिक मानते हैं तो अन्य पूर्ण आर्थिक समानता को प्राकृतिक समझते हैं। कुछ विद्वान् स्त्री-पुरुष की समानता का समर्थन करते हैं तो कुछ इसका विरोध । लाँस्की ने इसी बात को लक्ष्य करते हुए लिखा है कि “अधिकारों की कोई स्थाई या अपवर्तित सूची निर्मित नहीं की जा सकती।”
(3) अधिकारों की निरपेक्षता स्वीकार नहीं- हर सिद्धान्त के अनुसार, अधिकार व्यक्ति को प्रकृति की देन होने के कारण निरपेक्ष हैं और अधिकारों पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगाया जा सकता, लेकिन व्यवहार में स्वतन्त्रता और समानता के अधिकारों का प्रयोग प्रतिबन्धों की विद्यमानता में ही किया जा सकता है। प्रतिबन्ध के अभाव में स्वतन्त्रता उच्छृंखलता में परिणत हो जाती है और समानता एक कल्पना मात्र बनकर रह जाती है। इस प्रकार के निरपेक्ष अधिकार आवश्यक रूप से सम्पूर्ण समाज के हित को विरुद्ध होंगे।
(4) प्राकृतिक अधिकारों में पारस्परिक विरोध- प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास का दोष भी पाया जाता है। अधिकारों की निरपेक्षता को स्वीकार कर लेने पर स्वतन्त्रता और समानता के अधिकार परस्पर विरोधी हो जाती हैं और इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है।
(5) राज्य कृत्रिम संस्था नहीं- इस सिद्धान्त के अनुसार, राज्य एक कृत्रि संस्था है, जिसने शक्ति के आधार पर नागरिकों को अधिकारों से वंचित कर दिया है, किन्तु वास्तविकता इसके नितान्त विपरीत है। राज्य एक शाश्वत संस्था है जिसने अपने कानूनों द्वारा मानवीय अधिकारों का अपहरण नहीं वरन् रक्षा की है। वास्तव में, राज्य एक प्राकृतिक समुदाय है और कानूनों के बिना अधिकारों का अस्तित्व सम्भव नहीं है।
(6) सामाजिक मान्यता के अभाव में अधिकार की कल्पना सम्भव नहीं – इस सिद्धान्त में समाज से अलग रहकर अधिकारों की कल्पना की गयी है, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं है। समाज से अलग रहकर हमारे पास शक्तियाँ हो सकती हैं, अधिकार नहीं, क्योंकि बिना सामाजिक मान्यता के अधिकार का अस्तित्व सम्भव नहीं हो सकता। जैसा कि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि “अधिकारों की उत्पत्ति इसी तथ्य से हुई है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” वस्तुतः अधिकार तो व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला वह दावा है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।
महत्त्व – इस प्रकार अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त का जिस रूप में प्रतिपादन किया गया। है, उस रूप में वह सर्वथा अमान्य है। फिर भी इस रूप में प्राकृतिक सिद्धान्त को स्वीकार किया ना सकता है कि प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों के उपयोग से है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं जिनसे मनुष्य को वंचित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय के अमरीका, भारत, आदि देशो के संविधानों में मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गयी है, वह अधिकारों की इसी धारणा पर आधारित है। प्राकृतिक सिद्धान्त और मौलिक अधिकारों की धारणा में अन्तर केवल यही है कि मौलिक अधिकारों की धारणा में स्पष्ट रूप से यह समझ लिया गया है कि राज्य मानव अधिकारों का हनन नहीं, वरन् रक्षा करता है। अतः लॉर्ड के शब्दों में कहा जा सकता है कि “यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक अधिकार वे शर्तें हैं जो मानवीय संस्था द्वारा प्रदान की गयी हों अथवा नहीं, परन्तु जो व्यक्तित्व के विकास हेतु अत्यावश्यक हैं।” गिलक्राइस्ट इसी प्रकार की पुष्टि इन शब्दों में करता है “प्राकृतिक अधिकारों को जिस उचित अर्थ में लिया जा सकता है, वह केवल यही है कि मनुष्य की नीतिशास्त्र के अनुसार सच्चा मनुष्य बनने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, वह सब उसे अवश्य ही प्राप्त होना चाहिए।”
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।