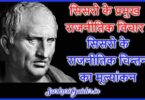अधिकार के प्रकार या अधिकारों का वर्गीकरण
साधारणतया अधिकार दो प्रकार के होते हैं- (1) नैतिक अधिकार और (2) कानूनी अधिकार।
(1) नैतिक अधिकार- नैतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका सम्बन्ध मानव के नैतिक आचरण से होता है। अनेक विचारकों के द्वारा इन्हें अधिकार के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि वे अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं। इन्हें धर्मशास्त्र, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता ।
(2) कानूनी अधिकार- ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दण्डनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। लीकॉक ने इन अधिकारों की परिभाषा करते हुए कहा है कि “कानूनी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो एक नागरिक को अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं तथा जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा प्रदान किये जाते हैं और रक्षित होते हैं।”
कानूनी अधिकार के दो भेद किये जा सकते हैं-
(1) सामाजिक या नागरिक अधिकार, (2) राजनीतिक अधिकार ।
(i) सामाजिक या नागरिक अधिकार – प्रमुख सामाजिक या नागरिक अधिकार निम्नलिखित है-
(1) जीवन का अधिकार- मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना अन्य किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अन्त न कर सके।
जीवन के अधिकार के अन्तर्गत ही आत्मरक्षा का अधिकार भी निहित है, इसका तात्पर्य यह हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर आघात किया जाता है तो सम्बन्धित व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और आत्मरक्षा के लिए निमित्त की गयी यह कार्यवाही अपराध की श्रेणी में नहीं आती है।
प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक आवश्यक अंग होता है और व्यक्ति का जीवन स्वंय अपने साथ-साथ सम्पूर्ण समाज की सम्पत्ति होती है, इसलिए जीवन के अधिकार में यह बात भी सम्मिलित है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का भी अन्त नहीं कर सकता है। अतः आत्महत्या एक दण्डनीय अपराध है। सैण्ट थॉमस एक्वीनास के शब्दों में, “आत्महत्या स्वयं अपने प्रति, समाज के प्रति और ईश्वर के प्रति एक अपराध है।”
(2) समानता का अधिकार – समानता का अधिकार एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है और इकसा तात्पर्य यह है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्त्व प्राप्त होना चाहिए और जाति, धर्म व आर्थिक स्थिति के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। समानता का अधिकार प्रजातन्त्र की आत्मा है और इसके निम्न भेद हैं
(क) राजनीतिक समानता का अधिकार- इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यतानुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। इस राजनीतिक समानता की प्राप्ति प्रजातन्त्रात्मक शासन की स्थापना और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था द्वारा ही सम्भव है। इसी में यह बात भी शामिल है कि न्याय और कानून की दृष्टि से भी सभी व्यक्ति समान समझे जाने चाहिए।
(ख) सामाजिक समानता का अधिकार- इसका तात्पर्य यह है कि समाज में धर्म, जाति, भाषा, सम्पत्ति, वर्ण या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्ति होने के नाते ही समाज में सम्मान प्राप्त होना चाहिए। डॉ. बेनीप्रसाद के शब्दों में, “सामाजिक समानता का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक के सुख का समान महत्त्व है तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधनमात्र नहीं समझा जा सकता है।” सामाजिक समानता की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।
(ग) आर्थिक समानता का अधिकार – वर्तमान समय में आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है मानव के आर्थिक स्तर में गम्भीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए और सम्पत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए। टॉनी के शब्दों में, “आर्थिक समानता का अर्थ एक ऐसी विषमता के अभाव से है जिसका उपयोग आर्थिक दबाव के रूप में किया जा लॉस्की के अनुसार इसका तात्पर्य ‘उद्योग में प्रजातन्त्र’ से है।
(3) स्वतन्त्रता का अधिकार – स्वतन्त्रता का अधिकार जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा समाज का विकास सम्भव नहीं है।
स्वतन्त्रता का तात्पर्य उच्छृंखलता या नियन्त्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। लॉस्की के शब्दों में, “इसका तात्पर्य उस शक्ति से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से बिना किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सके।” किसी बाहरी बन्धन के अपने जीवन का विकास कर सकें” स्वतन्त्रता के अधिकार के भेद निम्नलिखित हैं
(क) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना सामान्य जीवन विवेक के अनुसार व्यतीत कर सकें। मिल व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को अधिक महत्त्व देते हैं और इसे सर्वोत्तम सद्गुण मानते हैं। स्वतन्त्रता के इस रूप का बहुत प्रतिपादन करते हुए ‘मिल कहते हैं कि “स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु होता है।” व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही यह बात भी सम्मिलित है कि कानून का उल्लंघन किये बिना किसी व्यक्तिको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और न्याय द्वारा अभियोग की पुष्टि के बिना उसे बन्दी नहीं बनया जा सकता है।
(ख) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार- विचार स्वातन्त्र्य मानसिक और नैतिक उन्नति की सर्वोच्च शर्त है। मानव एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्तिका आत्मविकास एवं समाज की सम्पूर्ण उन्नति विचारों के आदान-प्रदान पर भी निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने और भाषण, लेख, आदि के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अन्तर्गत ही सम्पत्ति देने, आलोचना करने, लेखन एवं प्रशासन की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित हैं। सुकरात ने विचार स्वातन्त्र्य त्यागने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेयस्कर समझा था और मिल्टन, मिल, वाल्टेयर, लाँस्की, आदि सभी विद्वानों ने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का महत्त्व स्वीकार किया है। मिल्टन कहते हैं, “मुझे अपने अन्तरमन के अनुसार जानने की, बोलने की और तर्क करने की स्वतन्त्रता अन्य स्वतन्त्रताओं से अधिक प्रिय है।” मिल लिखते हैं, “यदि एक को छोड़कर समस्त मानव समुदाय एकमत हो, तो मानव समुदाय का उस व्यक्ति को चुप कराना उससे अधिक उचित नहीं है जितना उस व्यक्ति का, यदि उसके पास शक्ति हो, मानव समुदाय को चुपकराना।”
(ग) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का अधिकार – अन्तःकरण की स्वतन्त्रता या धार्मिक स्वतन्त्रता का अभिप्राय है कि व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का धर्म नहीं लादा जा सकता है। धर्म का सम्बन्ध व्यक्ति के अन्तःकरण से होता है और इस कारण इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का बाहरी दबाव नितान्त अनुचित है, किन्तु धार्मिकता की आड़ में अनाचार, अत्याचार या धार्मिक असहिष्णुता की आज्ञा नहीं जा सकती है। धार्मिक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में रूसो ने ठीक ही कहा है कि “सब धर्मों को, जो दूसरे धर्मों को सहन करते हैं, सहन किया जा सकता है। जब तक उसके मत नागरिकता के कर्तव्यों का विरोध नहीं करते।”
(घ) समुदाय निर्माण की स्वतन्त्रता का अधिकार- “संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूल मन्त्र है’ इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्मण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि वह जीवन के विविध क्षेत्रों में उन्नति करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समुदायों का निर्माण कर सके, लेकिन इस प्रकार के किसी भी संगठन को समाज-विरोधी या अनैतिक कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती है।
(ङ) नैतिक स्वतन्त्रता – एक व्यक्ति के पास उपर्युक्त सभी स्वतन्त्रताएँ होने पर भी यदि उसे नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। नैतिक स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोम लालच के कार्य कर सके। नैतिक स्वतन्त्रता नींव के उस पत्थर के समान है जिस पर जीवन का सम्पूर्ण भवन आधारित होता है और नैतिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक एवं सामाजिक स्वतन्त्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता।
(4) सम्पत्ति का अधिकार- मानव जीवन के लिए सम्पत्ति आवश्यक है। सम्पत्ति के अधिकार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि यह विचार मानव को उन्नति की ओर। प्रेरित करता है। सम्पत्ति के अधिकार का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गये धन को चाहे तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है और धन, जीवन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रक्षित इस सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये उससे छीना नहीं जा सकता है।
वर्तमान समय में सम्पत्ति के अधिकार को अनियन्त्रित रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका कारण यह है कि सम्पत्ति का अधिकार जहाँ एक ओर दया, दान, उदारता, स्नेह, कार्यक्षमता, आदि मानवीय गुणों की ओर प्रेरित करता है, वहाँ यह विषमता, भेदभाव, वैमनस्य और शोषण के दुर्गुणों का भी कारण बन जाता है। अतः जनकल्याण की दृष्टि से सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में लाँस्की ने लिखा है कि “सम्पत्ति का अधिकार तभी तक है जब तक कि मेरी सेवा की दृष्टि से उसका कुछ महत्त्व है—उस वस्तु पर मेरा स्वामित्व नहीं हो सकता, जिसका उत्पादन प्रत्यक्षतः किसी अन्य के श्रम से हुआ हो। मेरा किसी वस्तु का स्वामित्व न्यायपूर्ण नहीं हो सकता, यदि उसके परिणामस्वरूप मुझे अन्य व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है।” एक अन्य स्थान पर लॉस्की ही लिखते हैं कि “धनवान तथा निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका होता है। सम्पत्ति अकर्मण्यता को घोषित करती है। सम्पत्तिवान लोग रचनात्मक कार्यों में अपना समय नहीं लगाते। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति राजनीति में अवांछनीय रूप से धन का रौब पैदा करती है, जो कि अन्त में समस्त प्रशासन को दूषित कर देता है।” यह एक तथ्य है कि सम्पत्ति का अधिकार सामाजिक आवश्यकताओं से मर्यादित होता है।
(5) रोजगार का अधिकार – व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण-पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की सम्पत्ति होती है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी-न-किसी प्रकार का काम किये बिना प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक समझा जाता है। कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए और इस काम के बदले में व्यक्ति को उचित पारिश्रमिक प्राप्त होना चहिए। लाँस्की के शब्दों में, “अपना सर्वोत्तम रूप प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को काम करना चाहिए और काम के अभाव में उस समय तक के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए, जब तक किसी व्यवस्था में उसे पुनः काम करने का अवसर प्राप्त न हो, एक व्यक्ति को केवल काम का ही अधिकार नहीं, अपितु उसे कार्य के उपयुक्त मजदूरी का अधिकार होना। चाहिए।’
नैतिक रूप में वर्तमान समय के सभी राज्य इस प्रकार के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, किन्तु भारत जैसे अनेक राज्यों में आर्थिक साधनों के अभाव के कारण राज्य कानूनी रूप नागरिकों को अब तक इस प्रकार का अधिकार नहीं कर सका है।
(6) शिक्षा का अधिकार- शिक्षा मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास सम्भव है। अतः वर्तमान समाज में यह बात सामान्य है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान एवं निर्धन, दोनों ही वर्गों को शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए। वाचनालय, पुस्तकालय और संग्राहलयों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रारम्भिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप में व्यवस्था की जानी चाहिए।
राजनीतिक अधिकार – राजनीतिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रबन्धन में भाग लेते हैं। साधारणतया एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को निम्नलिखित राजनीतिक अधिकार प्राप्त किये जाते हैं
(1 ) मत देने का अधिकार – वर्तमान समय के विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रीय व्यवस्था सम्भव नहीं रही है और इसलिए प्रतिनिध्यात्मक प्रजातन्त्र के रूप में एक ऐसी व्यवस्था की गयी है और जिनमें जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और इन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य किया जाता है। इस प्रकार जनता मताधिकार के माध्यम से ही देश के शासन में भाग लेती है और मतदान को प्रजातन्त्र की आधारशिला कहा जा सकता है। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मताधिकार को अधिकाधिक व्यापक बनाने की है और इसलिए अधिकांश देशों में वयस्क मताधिकार को अपना लिया गया है।
(2) निर्वाचित होने का अधिकार – प्रजातन्त्र में शासक और शासित का कोई भेद नहीं होता और योग्यता सम्बन्धी कुछ प्रतिबन्धों के साथ सभी नागरिकों को जनता के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होता है। इसी अधिकार के माध्यम से व्यक्ति देश की उन्नति में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है।
(3) सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार— व्यक्ति को सभी सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और इस सम्बन्ध में योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर भेद नहीं किया जाना चाहिए।
(4) आवेदन-पत्र और सम्पत्ति देने का अधिकार- लोकतन्त्रीय शासन का संचालन जनहित के लिए किया जाए। अतः नागरिकों को अपनी शिकायतें दूर करने या शसन को आवश्यक सम्पत्ति प्रदान करने के लिए व्यक्ति या सामूहिक रूप से कार्यपालिका या व्यवस्थापिका अधिकारियों का प्रार्थना-पत्र देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इसके अन्तर्गत ही शासन की आलोचना का अधिकार भी सम्मिलित किया जाता है।
साधारण रूप से इस प्रकार के अधिकार देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं और देश में बसे हुए विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इन राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत ही की जा सकती है।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।