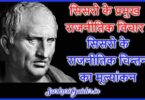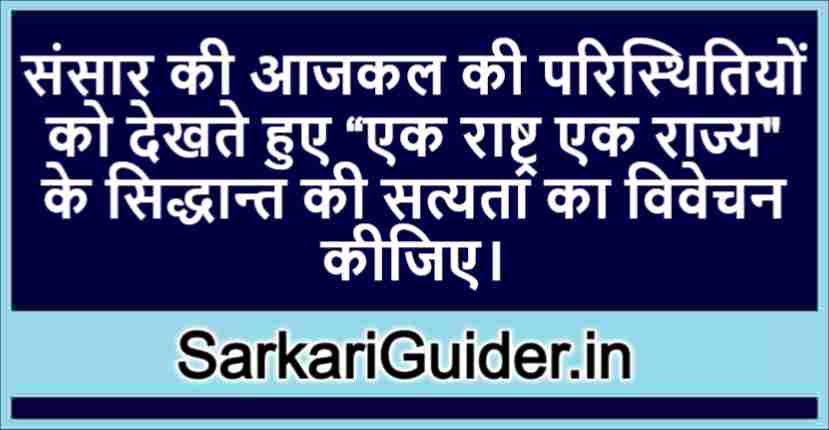
एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त की सत्यता
आधुनिक राष्ट्रवाद की विशेषता है कि अधिकांश जनता जो किसी राष्ट्र में राष्ट्रीयता का निर्माण कर लेती है वह या तो स्वतन्त्र होने या अपनी इच्छा के अनुसार अपने द्वारा निर्मित राज संगठन के अन्दर निवास करने की कामना करती है या, कम से कम यह चाहती है कि यदि इसे राष्ट्रीयता या, राष्ट्रीयताओं के साथ एक ही राज्य के अन्तर्गत संयुक्त कर दिया गया हो तो उसे अधिकाधिक राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए।” -गार्नर
‘एक राष्ट्र एक राज्य’ या राष्ट्रीयताओं एवं आत्मनिर्णय का सिद्धान्त – राष्ट्रीयताओं राज्यों के सिद्धान्त के अन्तर्गत राजनैतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयताओं में आत्म निर्णय का सिद्धान्त एक प्रमुख स्थान रखता है इस सिद्धान्त ने अनेक सिद्धान्तों को जन्म दिया है। वियना कांग्रेस 1815 और 1918 के वार्साई सन्धि के मूल सिद्धान्त के रूप में इस सिद्धान्त के अनेक राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण किया। प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोपीय पुनर्व्यवस्था के सम्बन्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने अपनी 14 सूत्रीय योजना में इस सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया। आधुनिक काल में ‘रेम्जे म्योर’ ने इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए लिखा है- “राष्ट्रीय विभाजन सीमा के संघर्ष द्वारा एक बार स्थापित होकर आश्चर्यजनक रूप से स्थायी होती हैं अतएव यदि एक बार यूरोप का पूर्ण एवं सन्तोषजनक विभाजन राष्ट्रीय आधार पर जाता है तो संघर्ष के अन्त की यथेष्ट आशा की जा सकती है। “
प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैण्ड और चेकोस्लोवाकिया देशों का निर्माण इसी आधार पर किया गया और द्वितीय महायुद्ध के बाद इण्डोनेशिया, हिन्द, चीन, घाना, कांगो, साइप्रस आदि राष्ट्रों को इसी सिद्धान्त पर स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन् 1947 में भारत का विभाजन आत्मनिर्णय के आधार पर किया गया।
राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के अधिकार का अर्थ यह है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपनी स्वतंत्रता के बारे में निर्णय करने का अधिकार है अर्थात् प्रत्येक राष्ट्रीयता को यह अधिकार है कि वह अपने राजनैतिक भविष्य का निर्णय स्वयं करें। उसके ऊपर बलात इच्छा निर्णय किसी प्रकार की शासन पद्धति को न थोपा जाए यदि विभिन्न राष्ट्रीयताओं को बलात् राष्ट्रीय संगठन के अन्तर्गत रखा जाए। तो वे कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकती है उसमें पारस्परिक आन्तरिक झगड़े उत्पन्न होते रहेंगे और उन्नति अवरुद्ध हो जायेगी।’
जे. एस. मिल ने कहा है कि सामान्यतः स्वतंत्र संस्थाओं की यह आवश्यक शर्त है कि अधिकांश जनता जो कि राष्ट्रीयता का निर्माण करती है वह स्वतंत्र होने तथा अपनी इच्छानुसार अपने द्वारा निर्मित राज्य संगठन के अन्दर निवास करने की कामना करती है या कम से कम चाहती है कि यदि उसे किसी राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयताओं के साथ ही एक ही राज्य के अन्दर संयुक्त कर दिया गया तो उसे अधिकाधिक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए।
इस सिद्धान्त के पक्ष में प्रमुख रूप से निम्न तर्कों को प्रस्तुत किया गया है-
1. प्रतिनिधि शासन प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक – इस सिद्धान्त का प्रबल समर्थक लोकतंत्र की सफलता के हित में इसे उचित मानता है। जब एक राष्ट्रीयता को स्वयं अपने भाग्य के निर्णय का अधिकार दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसका तात्पर्य जनता के शासन से ही होता है। इस प्रकार के शासन में हितों की एकता एक ही राष्ट्रीय राज्य से सम्भव है जैसा का मिल ने कहा है- “एक ही राष्ट्रीय राज्य में विचारों का यह आदान-प्रदान सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सकता है” ब्राइस ने इसी प्रकार लिखा है- “आत्मनिर्णय का सिद्धान्त उदारवाद और प्रजातंत्र की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीयताओं का प्रतीक है। “
मैकाइवर ने भी लिखा है- “इसने हमारे आधुनिक प्रजातंत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।”
2. अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान- एक राष्ट्रीय राज्य में अल्पसंख्यकों की कोई समस्या नहीं होती। अल्पसंख्यकों के साथ अहित नहीं हो पाता क्योंकि इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को अपने पृथक्-पृथक् राज्य मिल जाते हैं और वे सरलतापूर्वक अपना विकास कर सकते हैं।
3. स्वतंत्रता का परिचय – आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को स्वतंत्रता का परिचय भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त का अनुकरण करने पर उन सभी राष्ट्रीयताओं को स्वतंत्रता मिल जाती है जो साम्राज्य के घेरों में बंधी हुई है और इस प्रकार साम्राज्यवाद का अन्त सम्भव हो जायेगा।
4. राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक- इस सिद्धान्त की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि आन्तरिक मतभेदों का अभाव होने के कारण एक राष्ट्र अच्छी प्रकार से संगठित होता है जिससे राष्ट्रीय एकता तथा सुदृढ़ता की भावना जाग्रत होती है जिससे राष्ट्र सबल और मजबूत बनता है। इससे जनता में देशभक्ति की भावना बढ़ती है इसके आधार पर निर्मित राज्य में स्वावलम्बन की भावना का संचार होता है और जनता यथार्थ का अनुभव करती है।
राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के उपर्युक्त गुण होते हुए भी अनेक दोष पाये जाते हैं और विभिन्न तर्कों के आधार पर इस सिद्धान्त की आलोचना की जाती है—
1. यह तर्क सही नहीं है कि लोकतंत्र में विभिन्न राष्ट्रीयता सुखपूर्वक नहीं रह सकती। इंग्लैण्ड तथा स्विट्जरलैण्ड के लोकतंत्र पर्याप्त स्थायी तथा सफल सिद्ध हुए हैं यद्यपि दोनों राष्ट्रों में विभिन्न राष्ट्रीयताएँ निवास करती हैं और उन राष्ट्रीयताओं ने कभी भी अपने आत्म-निर्णय या पृथक राष्ट्रीय राज्य की भावना को व्यक्त नहीं किया है।
2. यह सिद्धान्त एकता के स्थान पर पृथक्तावादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है स्वयं यूरोप में जहाँ इसका प्रादुर्भाव हुआ था इसका अक्षरशः पालन नहीं किया गया। वर्तमान समय में सुदृढ़ राजनैतिक संगठनों के हेतु अपने राष्ट्रीयताओं के मध्य पृथक राष्ट्रीय राज्य निर्मित करने की उपेक्षा राजनीतिक एकता लाने तथा उनके सुदृढ़ राजनैतिक संगठन बनाने के उद्देश्य से संघवाद की प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है। ‘लार्ड कर्जन’ ने कहा है कि ‘प्राचीन काल में राष्ट्रीय आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का उद्देश्य एकता का संचार करना था आधुनिक काल में यह संघर्षों का द्योतक है।” इस दृष्टि से यह सिद्धान्त दोषपूर्ण है।
3. इस सिद्धान्त को सही-सही रूप में कार्यान्वित कर सकना भी अव्यावहारिक है। सही माने में किसी राष्ट्रीयता विशेष का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उदाहरण के लिए केवल धर्म के आधार पर हम यह निर्धारित नहीं कर सकते कि सिक्खों की अलग राष्ट्रीयता है या मुसलमानों की अलग राष्ट्रीयता है। आज के युग में या तो विभिन्न राष्ट्रीयताएँ मिलकर एक राष्ट्रीयता में परिणित हो चुकी हैं या विभिन्न तत्वों की दृष्टि से असंख्य राष्ट्रीयताओं का अस्तित्व है जिनके पृथक आत्म निर्णय की कल्पना की जा सकती है।
4. विश्व शान्ति के लिए उपयोगी है—विश्व शान्ति तथा अन्तर्राष्ट्रीयता के हित में भी इस सिद्धान्त का विरोध किया गया है। यह धारणा निर्मूल नहीं है कि राष्ट्र राज्य का सिद्धान्त विश्व बन्धुत्व को बढ़ाने की अपेक्षा पृथक्ता की भावना को बढ़ाता है इसका प्रमाण द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी, इटली तथा जापान के उग्र राष्ट्रवाद हैं जिन्होंने विनाशकारी युद्ध को भड़काया। ‘जोजेफ’ का विचार है कि “विश्व के मामलों में शान्ति एवं व्यवस्था का एक मात्र आशय इस तथ्य की मान्यता पर आधारित है कि राज्य के अन्दर सहयोग तथा एकता के साथ अनेक राष्ट्रीयताएँ निवास करें, साथ-साथ अपनी-अपनी जीवनचर्या भी बिताती रहें।
जोजेफ वे मत से “राजस्व तथा राष्ट्रत्व अलग-अलग चीजें हैं और राजस्व की समाप्ति होने पर भी राष्ट्रत्व का अस्तित्व बना रहता है।” इसके अनुसार यह बात स्पष्ट है कि एक राष्ट्र की सीमाओं के समकक्षीय होने का सिद्धान्त पूर्णतः अशुद्ध तथा तथ्यों से रहित है। ‘लार्ड एक्टन’ का भी मत है कि ‘सभ्यता के हित में अनेक राष्ट्रीयताओं को एक राज्य के अन्तर्गत रहना चाहिए जिससे कि निर्बल राष्ट्रीयताएँ सबलों के सम्पर्क में आने पर उन्नति कर सकें।” उसके मध्य एक दूसरे के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। लार्ड एक्टन ने ‘एक राष्ट्र एक राज्य’ के सिद्धान्त का उतना ही मूर्खतापूर्ण कहा है जितना कि समाजवाद का सिद्धान्त। इस प्रकार ‘जिमर्न’ ने भी कहा है कि “राष्ट्रीय राज्य का सिद्धान्त अन्ततोगत्वा हेनरी अष्टम् तथा लूथर चतुर्थ के सिद्धान्त की दिशा में पहुंच जायेगा।”
निष्कर्ष – इस सिद्धान्त के पक्ष-विपक्ष के गुण-दोषों में विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आत्म-निर्णय के सिद्धान्त का जहाँ अनेक तर्कों के आधार पर विरोध किया जाता है वहाँ यह भी माना जाता रहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपने राजनैतिक भविष्य निर्धारित करने तथा अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का अधिकार मिलना चाहिए। यदि एक ओर अन्तर्राष्ट्रीयता पर आधारित होने के कारण बहुराष्ट्रीय राज्य श्रेष्ठ है तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद तथा उपनिवेश की समाप्ति के लिए एक राष्ट्रीय राज्य का प्रतिपादन किया जाता है। इस सम्बन्ध में गार्नर ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हुए लिखा है- “जहाँ असन्तुष्ट राष्ट्रीयता किसी राज्य की जनता का कम से कम एक बड़ा भाग हो उसे प्रथम राजनीतिक संगठन का नैतिक आधार होना चाहिए।”
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।