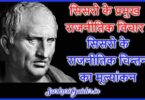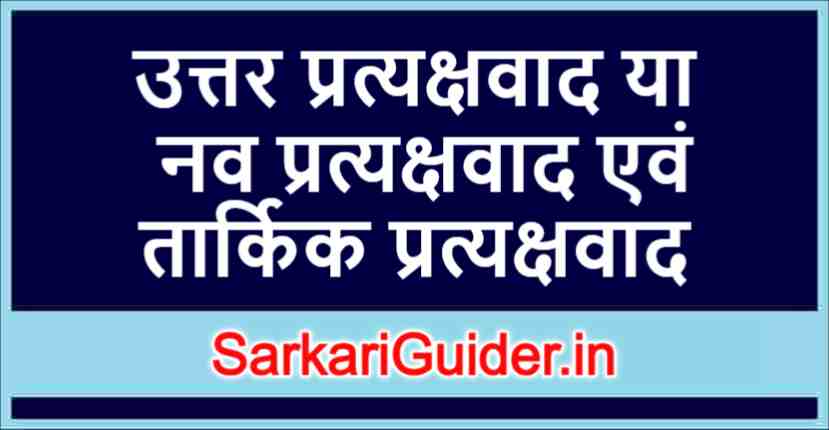
उत्तर प्रत्यक्षवाद या नव प्रत्यक्षवाद एवं तार्किक प्रत्यक्षवाद
नव प्रत्यक्षवाद और तार्किक प्रत्यक्षवाद
प्रत्यक्षवाद के परवर्ती समर्थकों ने तथ्य मूल्य-संबंध के बारे में कॉम्टे की मान्यताओं को स्वीकार नहीं किया। अतः बीसवीं शताब्दी के आरंभ में इस विषय पर जो नया दृष्टिकोण उभर कर सामने आया, उसे नव-प्रत्यक्षवाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद की संज्ञा दी जाती है। इस दृष्टिकोण के उन्नायकों में जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर (1864-1920) और ‘विएना सर्किल’ के सदस्यों का विशेष योगदान रहा है। मैक्स वेबर ने अपने प्रसिद्ध निबंध ‘साइंस पेज प वोकेशन’ (विज्ञानः एक व्यवसाय) (1919) के अंतर्गत यह विचार व्यक्त कियाः ” विज्ञान हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? शैक्षिक ज्ञान हमें सृष्टि के अभिप्राय की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं देता। इसके बारे में परस्पर-विरोधी व्याख्याओं में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता।” इसी तरह टी.डी. वेल्डन ने अपनी चर्चित कृति ‘वोकेबुलरी ऑफ पॉलिटिक्स’ (राजनीति की शब्दावली) (1953) के अंतर्गत वेबर की इस मान्यता को दोहराया कि कोई भी राजनीति दर्शन अपनी-अपनी अभिरूचि का विषय हैं। कोई व्यक्ति अपनी अभिरूचित बता तो सकता है, परंतु उस पर तर्क-वितर्क करने से कोई फायदा नहीं ।
तार्किक प्रत्यक्षवाद की बाकायदा एक आंदोलन का रूप देने में ‘विएना सर्किल’ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह संप्रदाय विएना विश्वविधायल के मोरिट्ज श्लिक (1882-1936) के नेतृत्व में 1920 के दशक में विकसित हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविधालय में यह लुड्विख विट्जेंस्टाइन में यह ए.जे.एयर (1910-89) के नेतृत्व में आगे बढ़ा। तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने यह तर्क दिया कि चिंतनमूलक दर्शन केवल ऐसे प्रश्नों से सरोकर रखता है जिन्हें अनुभवमूलक दृष्टि से नहीं परखा जा सकता— जैसे कि सत्य, शिव और सुंदर क्या हैं? उनका कहना था कि जिन प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर नहीं दिया जा सकता, ऐसे प्रश्न ही निरर्थक हैं, वे केवल छदप्रश्न हैं। हमें केवल उसी ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए जिसे प्राकृतिक विज्ञान की कठोर पद्धति के द्वारा प्राप्त किया गया हो। अतः उन्होंने तत्त्वमीमांस में निहित ज्ञान का विशेष रूप से खंडन किया।
समालोचना
यह सच है कि वैज्ञानिक पद्धति से सामाजिक जीवन के लिए उपयुक्त मूल्यों और लक्ष्यों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये नैतिक निर्णय के विषय हैं; वैज्ञानिक निर्णय के विषय नहीं । परंतु सामाजिक जीवन के चलाने के लिए नैतिक निर्णय भी उतने जरूरी हैं। राजनीति-वैज्ञानिक इस विषय के अपने विचारक्षेत्र से बाहर मानते हुए अपने महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व से मुँह नहीं मोड़ सकते। यदि वे इन समस्याओं से दूर भागेंगे तो इनका निर्णय किसी और के हाथो में चला जाएगा। इससे समाज को भारी क्षति पहुँच सकती है। अतः उत्तर-व्यवहारवाद के अंतर्गत राजनीति वैज्ञानिकों से यह मांग की जाती है कि उन्हें सामाजिक जीवन के लक्ष्यों और मूल्यों से अवश्य सरोकार रखना चाहिए।
समकालीन चिंतन में आलोचनात्मक सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्यक्षवाद पर विशेष रूप से प्रहार किया गया है। हर्बर्ट माक्यूजे (1898-1979) तर्क दिया है कि आज के युग में सामाजिक विज्ञान की भाषा को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने की कोशिश हो रही है ताकि मनुष्य अपने सोचने के ढंग से ही यथास्थिति का समर्थक बन जाए। इस तरह वैज्ञानिक भाषा को आलोचनात्मक दृष्टि से रिक्त किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, चुनावों के अध्ययन में हम केवल निरीक्षण और परिमापन को अपने अन्वेषण का विषय बनाकर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देते कि स्वयं चुनाव की वर्तमान प्रक्रिया लोकतंत्र के आदर्श को कितना सार्थक करती है? प्रत्यक्षवाद से प्रेरित अनुसंधान में सामाजिक प्रक्रियाओं के आलोचनात्मक विश्लेषण की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती । वैज्ञानिक ज्ञान स्वयं अपनी प्रामाणिकता का दावा करता है। केवल वैज्ञानिक पद्धति से ही उसका खंडन किया जा सकता है। दूसरी ओर, सामाजिक ज्ञान केवल व्याख्या और कार्रवाई का एक विकल्प प्रस्तुत करता है। इसमें अन्य विकल्पों के साथ तुलना की गुजाइश हमेंशा बनी रहती है।
यदि सामाजिक ज्ञान भी वैज्ञानिक ज्ञान की तरह अपनी प्रामाणिकता का दावा करने लगेगा तो वह आलोचना का विषय नहीं रह जाएगा, और अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प के चयन की संभावना नहीं रह जाएगी। इस क्षेत्र में प्रत्यक्षवाद को अपना लेने पर सामाजिक विज्ञान सामाजिक अन्वेषण का साधन नहीं रह जाएगा बल्कि सामाजिक नियंत्रण का साधन बन जाएगा।
सामाजिक जीवन के गुणात्मक उत्कर्ष के लिए मूल्यों के प्रति सजगता जरूरी है। मूल्यों का सार्थक विश्लेषण मुक्त वातावरण की मांग करता है। समकालीन राजनीति-सिद्धांत मूल्यपरक कथन को निरर्थक नहीं मानता। राजनीति विज्ञान का ध्यये केवल वस्तुस्थिति का विवरण देना है, उसका मूल्यांकन करना नहीं परंतु राजनीति- सिद्धांत वस्तुस्थिति को किन्ही आदर्शो और मूल्यों की कसौटी पर परखता है, और उसकी त्रुटियों को दूर करने के उपाय भी सुझाता है। वस्तुतः मूल्यों राजनीति-सिद्धांत का मुख्य सरोकार इसलिए है ताकि वह वस्तुस्थिति का मूल्यांकन और आलोचना कर सके। देखा जाए तो राजनीति-दर्शन का उदय ही इसलिए हुआ कि कुछ सजग विचारकों ने अपने समय की राजनीति को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा और उसकी त्रुटियों का प्रबल विरोध किया। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने ‘सत्ताधारी के प्रति सत्य बोलने’ का बीड़ा उठाया, और इसके लिए उसे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा। सच्चे राजनीति – दार्शनकि सदैव मत विरोधी रहे हैं। इनसे बड़े-बड़े तानशाह भी डरते हैं। 1962 में जब म्यांमार (तत्कालीन बर्मा) में जनरल ने विन ने प्रधान मंत्री ऊ नू को हटाकर सैनकि अधिनायतंत्र स्थापित कर दिया तब उसने अपने देश के विश्वविधालयों और कॉलेजों में राजनीति विज्ञान के विभागों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि राजनीति- सिद्धांत का अध्ययन भी इन्हीं विभागों में होता था। अतः डांटे जमीन का यह कथन बहुत सटीक है: “राजनीति- सिद्धांत सचमुच राजनीति का आलोचनाशास्त्र है, और कुछ नही।” (बियोंड आइडियोलॉजी – द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी विचारधारा से परे राजनीति-सिद्धांत का पुनरूथान) (1967)।
वैज्ञानिक पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वह संचित ज्ञान होता है। इसमें प्रत्येक नया सिद्धांत अपने पूवर्वती सिद्धांत का उन्नत रूप होता है, अतः किसी भी घटना के संबंध में यहां नवीनतम सिद्धांत मान्य होता है जो पुराने सिद्धांत को अमान्य बना देता है। यदि किन्हीं नए तथ्यों का निरीक्षण करने पर प्रचलित सिद्धांत उनकी व्याख्या देने में असमर्थ सिद्ध होता है तो इस सिद्धांत का संशोधन जरूरी हो जाता है। दूसरी ओर मूल्यपरक कथन पर यह बात लागू नहीं होती है। इसमें मतभेद की गुजाइश बनी रहती है, और नया या पुराना होने के कारण किस कथन को मान्य या अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। उदाहरण के लिए, राजनीतिक दायित्व के आधार या सीमाओं के बारे में या न्याय के स्वरूप के बारें में निरंतर वाद-विाद चला आ रहा है, और चलता रहेगा। इन समस्याओं के बारे में किसी भी दृष्टिकोण को अंतिम रूप से मान्य नहीं माना जा सकता।
मूल्यपरक कथन के बारे में तीन प्रकार की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं :
(1) एक दृष्टिकोण यह है कि मूल्य व्यक्तिगत अधिमान्यता का विषय है; किसे क्या अच्छा लगता है या नहीं लगता- इस पर बहस बेकार है। यह दृष्टिकोण मूल्यों के विवेचन को राजनीति सिंद्धात के क्षेत्र के बाहर निकालने की वकालत करता है;
(2) दूसरा दृष्टिकोण मूल्य को ‘विचारधारा’ का विषय मानता है। इसके अनुसार, मूल्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि वह सत्तारूढ़ वर्ग या विरोधी वर्ग के अपने-अपने हितों के अनुरूप किसी प्रचलित या प्रस्ताति व्यवस्था को उचित ठहराने का प्रयास है। मार्क्स के अनुसार, विचाराधार शासक वर्ग के निहित स्वार्थों को प्रतिबिंबित करती है; अतः वह ‘मिथ्या चेतना’ को व्यक्त करती है। यह दृष्टिकोण भी प्रचलित मूल्यों के विश्लेषण को प्रायः निरर्थक समझता है;
(3) तीसरा दृष्टिकोण यह है कि परस्पर विरोधी मूल्यों और विचाराधाराओं का उपयुक्त विश्लेषण करके वस्तुपरक का पता लगाने की कोशिश कर सकते है। कार्ल मैन्हाइम (1893 1947) ने यह आशा व्यक्त की है कि भिन्न-भिन्न विचारधार रखने वाले वर्गों के बीच में यह बुद्धिजीवियों के एक ऐसे ‘मुक्त विचरणशील स्तर’ का अस्तित्व संभव है जो अपनी-अपनी सामाजिक स्थिति से निर्लिप्त होकर तटस्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये लोग शुरू-शुरू में स्वीकार करके चलेंगे कि उनका अपना-अपना दृष्टिकोण उनकी पृथक्-पृथक् सामाजिक स्थिति के साथ जुड़ा है; इसलिए वह अधूरा है। अतः वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह वे वर्तमान ऐतिहासिक परिस्थिति के बारे में संशलिष्ट सामान्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे जहां आकर उनके आपसी मतभेद मिट जाएगे।
कार्ल पॉपर (1902-94) में अपनी विख्यात कृति ‘द ओपेन सोसायटी एंड इट्ज एनिमीज’ (मुक्त समाज और उसके दुश्मन) (1945) के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि विचारधारा केवल सर्वाधिकारवादी समाज में पाई जाती है, क्योंकि वहां सब मनुष्यों को एक ही सांचे में ढालने की कोशिश की जाती है; मुक्त समाज में उसके प्रयोग की कोई गुजाइश नहीं है, क्योंकि उसमें लोग प्रचलित संस्थाओं और शक्ति-संरचनाओं की आलोचना करने के लिये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं।
अतः मूल्यों का सार्थक विश्लेषण मुक्त वातावरण की मांग करता है। यह बात याद रखने की है कि मूल्यों का विश्लेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्य-निर्णय वैज्ञानिक पद्धति का विषय नहीं है – यह इसका गुण है, त्रुटि नहीं। मूल्यों के सार तत्त्व को पहचानने के लिए विवेक-बुद्धि की आवश्यकता है; वैज्ञानिक प्रक्रिया इसके लिए पर्याप्त नहीं है। विवेकशील मनुष्य सहिष्णुता के आधार पर परस्पर संवाद स्थापित करके सहमति पर पहुँच सकते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति या समूह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने सत्य को पा लिया है। यदि ऐसा होगा तो मूल्यों की तलाश खत्म हो जाएगी और तथाकथित सत्य को निर्ममतापूर्वक लागू करना ही हमारा कर्तव्य रह जाएगा। इसका परिणाम होगा— अवरुद्ध समाज और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था जिसमें मनुष्य की स्वतंत्रता का दमन कर दिया जाएगा।
मूल्यों के प्रति उदार दृष्टिकोण की यही मांग है कि समाज में वैकल्पिक कारवाई की गुंजाइश लगातार बनी रहे; व्यक्ति को अनेक विकल्पों में से चयन का पूरा अवसर रहे। इसका अर्थ होगा – एक मुक्त, बहुलवादी समाज। इसमें वैकल्पिक कारवाई के गुण-दोषों पर मुक्त चर्चा की अनुमति रहेगी; प्रत्येक समूह को अपने-अपने दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक आधार सामग्री जुटाने और उसका प्रयोग करने में अभिरुचि रहेगी। भिन्न-भिन्न प्राक्कल्पनाओं की जाँच के लिए तर्कसंगत मानदंडों की तलाश की जाएगी। इस तरह वैज्ञानिक ज्ञान और मूल्य-निर्णय के बीच गहरी खाई नहीं खोदी जाएगी बल्कि इन दोनों के बीच संपर्क सेतु का निर्माण होगा।
संक्षेप में, राजनीति – सिद्धांत की सार्थकता इस बात में है कि वह सार्वजनिक जीवन के लक्ष्य निर्धारित करे, और ऐसी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का पता लगाए जो उन लक्ष्यों की सिद्धि में सहायक हों। ज्ञान-विज्ञान की कोई अन्य शाखा यह कार्य नहीं करती। राजनीति – सिद्धांत के विचारक्षेत्र में विज्ञान और दर्शन का जैसा मणि-कांचन संयोग देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू ने राजनीतिशास्त्र को ‘परन विद्या’ या ‘सर्वोच्च विज्ञान’ की संज्ञा इसलिए दी थी क्योंकि यह अन्य सब विद्याओं की उपलब्धियों को सद्जीवन की सिद्धि के लिए नियोजित करता है।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।