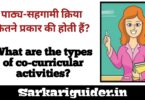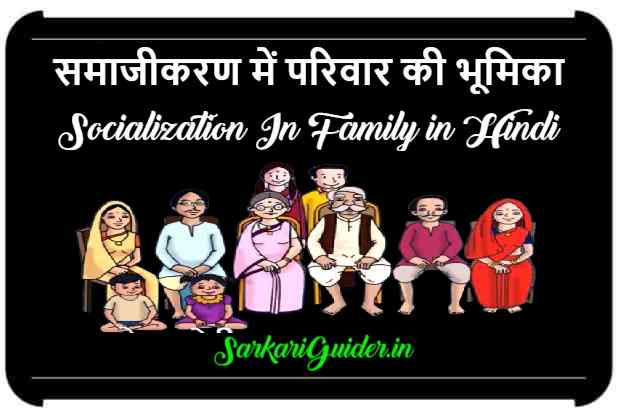
समाजीकरण में परिवार का योगदान | Socialization In Family
समाजीकरण में परिवार का योगदान- समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु आगे चलकर समाज का एक उत्तरदायी सदस्य बनता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात बालक का पालन-पोषण कैसे किया जाए कि वह समाज का एक योग्य सदस्य कहलाए। समाजीकरण उन सभी प्रयासों के सामूहिक रूप से बोला जाता है जिसका उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति में जो मान्यता है उनका अनुसरण करते हुए वह सफल नागरिक बने। अतः कह सकते है कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के द्वारा प्रदान की गई सामाजिक सांस्कृतियों को ग्रहण करने से है साथ ही समाज के कर्तव्य का पालन कते हुए समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनने से है। सरल शब्दों में बोला जा सकता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसे समाजीकरण कहते हैं।
समाजीकरण की परिभाषा
जॉनन के अनुसार, “समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है।”
समाजीकरण की प्रक्रिया वैसे तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, जो बालक के विकास को प्रभावित करी है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है-
परिवार का योगदान समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, यहीं से बालक सर्वप्रथम समाजीकरण आरम्भ करता है। इसी कारण से परिवार बालक का सर्व प्रथम पाठशाला कहा जाता है। परिवार ही वो जगह है जहां से बालक आदर्श नागरिक का पाठ सीखता है। बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं-
(1) माँ की भूमिका- बालक का परिवार में सबसे घनिष्ठ सम्बन्ध माँ से होता है। माँ करती तो उसका प्रभाव यह होता है कि बालक का समाजीकरण उचित प्रकार से नहीं होता।
(2) अधिक लाड़- प्यार- देखा गया है कि परिवार द्वारा आवश्यकता से अधिक प्यार करने से और उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करने देते जिस कारण से उनका समीकरण एक जाता है या ठीक ढंग से नहीं हो पाता जिसके परिणामस्वरूप बालक बिगड़ जाता है।
(3) माता-पिता का आपसी सम्बन्ध- बालक के समाजीकरण में माता-पिता का विशेष महत्व होता है। जैसे कि देखा गया है कि जिन परिवार में माता-पिता का आपसी सम्बन्ध अच्छे होते हैं उन परिवार का समाजीकरण उचित ढंग से होता है इसके विपरीत जिन परिवार में माता-पिता आपस में झगड़ते हैं इसके कारण बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे उनका समाजीकरण विकृत हो जाता है, क्योंकि आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण माता-पिता बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते।
(4) माता-पिता का बच्चे के साथ सम्बन्ध- माता-पिता जब बच्चों को उचित स्नेह देते हैं तो उनमें अच्छे सामाजिक गुण पैदा हो जाते हैं। यदि बच्चों को माता-पिता का उचित प्यार और सुरक्षा नहीं मिलता है तो उनका सामाजिक विकास अच्छे ढंग से नहीं होता। वे पूर्ण रूप से माता-पिता पर निर्भर हो जाते हैं। इसके विपरीत अगर बच्चों को कम स्नेह और प्यार मिलता है, उनमें बदला लेने की भावना विकसित हो जाती है। इस कारण से बालक कई बार बाल-अपराधी भी बन जाते हैं।
(5) बच्चों का अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध- बच्चे के परिवार के सम्बन्धियों का भी बच्चे के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चे के दादा-दादी, चाचा-चाची, मौसा-मौसी तथा अन्य परिवार के सगे-सम्बन्धियों के साथ सम्बन्ध कैसा है? ये भी बालक के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
(6) परिवार की आर्थिक नीति- यह भी देखा गया है कि अगर पारिवारिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो ये भी बालक के समाजीकरण में बाधा पहुँचाती है, क्योंकि बालक के पालन-पोषण में बच्चों को वो आर्थिक सुख-सुविधाएँ नहीं मिल पाती जो एक अच्छे आर्थिक परिवार के बच्चे को मिलती है। अतः इनसे बालक में सहनशीलता, परिश्रम करने वाले गुण विकसित होते हैं।
(7) परिवार की बनावट- परिवार दो प्रकार के होते हैं- (अ) संयुक्त परिवार तथा (ब) असंयुक्त परिवार।
संयुक्त परिवार तथा असंयुक्त परिवार ये दोनों ही समाजीकरण को अपने-अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। संयुक्त परिवार के बालक प्रायः सहनशील, सहानुभूतिपूर्ण, कम स्वार्थी होते हैं, दूसरी तरफ असंयुक्त पविार या छोटे परिवार वाले स्वार्थी होते हैं।
संक्षेप में कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में बहुत सी संस्थाएँ योगदान देती हैं फिर भी परिवार में योगदान सबसे ऊपर है क्योंकि समाजीकरण की पहली शिक्षा बच्चा परिवार के द्वारा ही सीखता है। परिवार के बाद बच्चा स्कूल द्वारा समाजीकरण करना सीखता है,परन्तु समाजीकरण में शिक्षा में परिवार की महांत्वता को नकारा नहीं जा सकता।
- समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा सहायक अभिकरण
- समाजीकरण के सिद्धांत | Theories of Socialization in Hindi
- मीड का समाजीकरण का सिद्धांत
- दुर्थीम का समाजीकरण का सिद्धांत
- कूले का समाजीकरण का सिद्धांत
- फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत
Important Links
- विद्यालय संगठन के उद्देश्य एंव इसके सिद्धान्त | Objectives and Principle of School Organization
- विद्यालय प्रबन्ध का कार्य क्षेत्र क्या है?विद्यालय प्रबन्ध की आवश्यकता एवं वर्तमान समस्याएँ
- विद्यालय संगठन का अर्थ, उद्देश्य एंव इसकी आवश्यकता | Meaning, Purpose and Need of School Organization
- विद्यालय प्रबन्धन का अर्थ, परिभाषा एंव इसकी विशेषताएँ | School Management
- विद्यालय प्रबन्ध के उद्देश्य | Objectives of School Management in Hindi
- विद्यालय प्रबन्धन की विधियाँ (आयाम) | Methods of School Management (Dimensions) in Hindi
- सोशल मीडिया का अर्थ एंव इसका प्रभाव | Meaning and effects of Social Media
- समाचार पत्र में शीर्षक संरचना क्या है? What is the Headline Structure in a newspaper
- सम्पादन कला का अर्थ एंव इसके गुण | Meaning and Properties of Editing in Hindi
- अनुवाद का स्वरूप | Format of Translation in Hindi
- टिप्पणी के कितने प्रकार होते हैं ? How many types of comments are there?
- टिप्पणी लेखन/कार्यालयी हिंदी की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।
- प्रारूपण लिखते समय ध्यान रखने वाले कम से कम छः बिन्दुओं को बताइये।
- आलेखन के प्रमुख अंग | Major Parts of Drafting in Hindi
- पारिवारिक या व्यवहारिक पत्र पर लेख | Articles on family and Practical Letter
- व्यावसायिक पत्र की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- व्यावसायिक पत्र के स्वरूप एंव इसके अंग | Forms of Business Letter and its Parts
- व्यावसायिक पत्र की विशेषताएँ | Features of Business Letter in Hindi
- व्यावसायिक पत्र-लेखन क्या हैं? व्यावसायिक पत्र के महत्त्व एवं उद्देश्य
- आधुनिककालीन हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ | हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का परिचय
- रीतिकाल की समान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी के रीतिबद्ध कवियों की काव्य प्रवृत्तियाँ
- कृष्ण काव्य धारा की विशेषतायें | कृष्ण काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ
- सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं | सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
Disclaimer