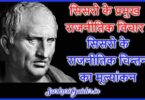हर्बर्ट साइमन के निर्णयन प्रक्रिया
साइमन के लिए प्रशासन ‘कार्य कराने’ की कला है। उन्होंने उन प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया, जिनसे कार्यवाही सुनिश्चित हो। वह कहते हैं कि प्रशासनिक विश्लेषण मे उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है जो कार्यवाही से पहले किया जाना है। निर्णय लेना चयन की वह प्रक्रिया है जिस पर कार्यवाही आधारित होती है। साइमन ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस आयाम को भली प्रकार समझने के अभाव में प्रशासन का अध्ययन अधिकांश रूप में अपर्याप्त रहेगा, क्योंकि यही संगठन में व्यक्ति के व्यवहार को सुस्थित करता है। व्यवहारवादी उपागम में कार्यवाही से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है, इसे
निर्णय लेने की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। साइमन ने इस बात पर बल दिया है कि निर्णय से अभिप्राय ‘तथ्यों’ एवं ‘मूल्य’ तत्त्वों का उचित योग होता है। ‘तथ्य’ से अभिप्राय है कि कोई वस्तु क्या है, क्या थी अथवा क्या रही है। तथ्य सच्चाई की अभिव्यक्ति है। इसके विपरीत, ‘मूल्य’ से तात्पर्य पसन्दगी से है। मूल्य वरीयता की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए यह तथ्य पर आधारित नहीं होती। साइमन के अनुसार प्रत्येक निर्णय अनेक तथ्यों और एक या अनेक मूल्य वक्तव्यों का परिणाम होता है। विकल्प या निर्णय में तथ्य तथा मूल्य दोनों शामिल होते हैं। ये किसी निर्णय में सम्मिलित नैतिक एवं तथ्यपरक तत्वों के विश्लेषण की कसौटियों को स्पष्ट करते हैं। साइमन ने उदाहरण दिया है कि मानो एक सेनापति आक्रमण की पद्धति के बारे में निर्णय करना चाहता है। वह इस मूल्य वक्तव्य से शुरू करता है, ‘मुझे आक्रमण करना चाहिए।’ यह ‘मूल्य’ वक्तव्य है। इसके विपरीत तथ्य वक्तव्य हैं ‘अचानक आक्रमण ही सफल होता है। यह तथ्य अनेक पूर्व अनुभवों पर आधारित हैं। इस ‘तथ्यं’ एवं ‘मूल्य’ सम्बन्धी कथनों को संयुक्त करने पर ‘निर्णय’ सम्भव होता है। इस प्रकार हर निर्णय ‘तथ्य कथनों’ एवं ‘मूल्य कथनों’ के संयोग का परिणाम है।
साइमन के अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं, परन्तु व्यक्ति को छँटनी की प्रक्रिया के माध्यम से केवल एक ही विकल्प चुनना होता है।
साइमन का मत है कि ‘निर्णय’ का अर्थ विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करना है। जब कोई समस्या सामने होती है, तो उसके विभिन्न विकल्प होते हैं। निर्णयकर्त्ता को अधिकतम लाभ या वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें से चयन करना पड़ता है। मानव की बुद्धिमत्ता इसमें है कि वह ऐसे विकल्प का चुनाव करे जिससे अधिकतम सकारात्मक तथा न्यूनतम नकारात्मक परिणाम निकले। इस दृष्टि से साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया को निम्न तीन चरणों में बाँटा है-
(i) अन्वेषण क्रिया–निर्णयन के इस प्रारम्भिक चरण में यह पता किया जाता है कि कब और कहाँ निर्णय की आवश्यकता होती है। साथ ही, इनमें निर्णय की उपयुक्त दशाओं के लिए बाह्य एवं आन्तरिक वातावरण की खोज की जाती है। इसमें संगठन की आन्तरिक नीतियों, प्रबन्धकीय व्यवहार एवं चिन्तन, संगठनात्मक, लक्ष्यों, मूल्यों व दर्शन के साथ-साथ बाह्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों, सामाजिक प्रारूपों, अभिवृत्तियों आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।
(ii) डिजाइन क्रिया- इस चरण में विभिन्न सम्भावित क्रियाविधियों का विकास एवं विश्लेषण किया जाता है। कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है।
(iii) चयन क्रिया–निर्णयन प्रक्रिया के तीसरे अन्तिम चरण में समस्त उपलब्ध क्रियाविधियों में से श्रेष्ठ क्रियाविधि का चयन किया जाता है। यह चयन विभिन्न विकल्पों की पारस्परिक तुलना एवं विश्लेषण के आधार पर किया जाता है।
साइमन अनुसार निर्णय निर्माण तार्किक (विवेकशीलता) चयन पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तार्किकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि यह मूल्यों की किसी प्रणाली के सन्दर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा सम्बन्ध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। कोई निर्णय तभी औचित्यपूर्ण या तार्किक (rational) माना जाता है जबकि इसके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चयन किया जाता है। साइमन लिखते हैं कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय का सही होना एक सापेक्षिक बात है-यह तभी सही होता है जबकि यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों का चुनाव करता है। साइमन पूर्ण तार्किकता की अवधारणा को नकारते हैं, क्योंकि यह अतार्किक मान्यताओं पर आधारित पूर्ण तार्किकता इस विश्वास पर आधारित है कि निर्णयकर्त्ता सर्वदर्शी है तथा उसे सभी प्राप्त विकल्पों तथा उनके परिणामों का ज्ञान है। दूसरे यह भी मान्यता है कि निर्णयकर्ता के पास असीमित कम्प्यूटरीय योग्यता है। अन्त में उसका विश्वास है कि निर्णयकर्ता में सभी सम्भावित परिणामों को एक व्यवस्था में रखने की क्षमता है। साइमन का कहना है कि ये सभी मान्यताएँ मौलिक रूप से गलत है। कौशलों, आदतों, मूल्यों तथा ध्येय की अवधारणा तथा अपने कार्य के संगत ज्ञान की सीमा के रूप में निर्णयकर्त्ता की अनेक सीमाएँ हैं। इसलिए साइमन का कहना है कि संगठन को पूर्ण तार्किकता की अवधारणा के साथ नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसे ‘सीमित तार्किकता’ के आधार पर कार्य करना चाहिए। साइमन के केवल ‘मर्यादित विवेकशीलता’ के आधार पर ही कार्य करता है। साइमन प्रशासनिक व्यवहार में अनुसार व्यक्ति पूर्ण विवेकशीलता के विचार को नकारता है। उसके अनुसार मानवीय व्यवहार न तो पूर्ण विवेकशील (तार्किक) होता है और न ही पूर्ण गैर-विवेकशील (अतार्किक) होता है वरन् यह ‘मर्यादित विवेकशील’ होता है। इसी सीमित तार्किकता के सन्दर्भ में साइमन तुष्टिकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। तुष्टिकरण शब्द ‘तुष्टि’ तथा ‘पर्याप्तता’ शब्दों से बना है। चूँकि पूर्ण तर्कसंगतता असम्भव है इसलिए कार्यकारी एक काफी अछे चयन से सन्तुष्ट होता है।
साइमन की यह भी मान्यता है कि सभी विकल्पों और उनके परिणाम को जानने में लोगों की योग्यता सीमित है और यह सीमा बन्धन पूर्णतः तर्कसंगत निर्णय को असम्भव कर देता है। चूँकि लोगों को भावी घटनाओं के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है, इससे वे अपने सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं। सीमित जानकारी के कारण लोग ऐसे विकल्प को चुन लेते हैं जो बिल्कुल परिपूर्ण न होकर साधारणतया ठीक होते हैं। ऐसे निर्णयों को साइमन ने ‘सन्तोषजनक निर्णय’ कहा है। साइमन लिखते हैं कि प्रबन्धक सदैव ‘अनुकूलतम समाधानों’ की खोज कर सकते हैं, किन्तु ‘पर्याप्त रूप से ठीक’ समाधानों से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की सीमाओं के कारण प्रबन्धकों का व्यवहार ‘उच्चतम’ न होकर केवल ‘सन्तोषप्रद’ ही हो जाता है।
साइमन ‘संयोजित’ तथा ‘असंयोजित’ निर्णयों में स्पष्ट अन्तर करते हैं। संयोजित निर्णय वे हैं जो स्वरूप से दुहराये जाने वाले तथा आम होते हैं। ऐसे निर्णयों के लिए निश्चित प्रक्रिया बनायी जा सकती हैं। प्रत्येक निर्णय पर अलग से विचार करना आवश्यक नहीं। ऐसे निर्णय में गणितीय मापांक तथा कम्प्यूटर निर्णयकर्ता को तार्किक निर्णयों को लेने में मदद कर सकते हैं। इसके विपरीत, असंयोजित निर्णय नये तथा अनबद्ध होते हैं। कोई पहले से तैयार पद्धतियाँ उपलब्ध नहीं होती तथा प्रत्येक प्रश्न या मसले पर अलग से विचार करना होता है।
साइमन के अनुसार निर्णय कार्यों का विशिष्टीकरण मुख्यतः निर्णयन केन्द्रों से तथा निर्णयन केन्द्रों की और पर्याप्त संचार मार्गों के विकास पर निर्भर करता है। अतः संगठन में औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार सूत्र होने चाहिए।
किसी परिणाम से सही अनुमान के लिए भविष्य में दृष्टिपात करने की क्षमता होनी चाहिए। सापेक्ष दृष्टि से उचित निर्णय एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कुछ विकल्प और उनके कुछ परिणाम ज्ञात होते हैं और उनमें से चयन किया जाता है। साइमन के अनुसार निर्णय लेने के सम्बन्ध में मनुष्य के वास्तविक आचरण का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- निर्णयन का अर्थ एवं परिभाषा | निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण
- लोक प्रशासन का अर्थ | लोक प्रशासन की परिभाषाएँ
- लोक प्रशासन कला अथवा विज्ञान । लोक प्रशासन की प्रकृति
Important Links
- मैकियावेली अपने युग का शिशु | Maikiyaveli Apne Yug Ka Shishu
- धर्म और नैतिकता के सम्बन्ध में मैकियावेली के विचार तथा आलोचना
- मैकियावेली के राजा सम्बन्धी विचार | मैकियावेली के अनुसार शासक के गुण
- मैकियावेली के राजनीतिक विचार | मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की मुख्य विशेषताएँ
- अरस्तू के परिवार सम्बन्धी विचार | Aristotle’s family thoughts in Hindi
- अरस्तू के सम्पत्ति सम्बन्धी विचार | Aristotle’s property ideas in Hindi
- प्लेटो प्रथम साम्यवादी के रूप में (Plato As the First Communist ),
- प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ (Features of Plato’s Education System),
- प्लेटो: साम्यवाद का सिद्धान्त, अर्थ, विशेषताएँ, प्रकार तथा उद्देश्य,
- प्लेटो: जीवन परिचय | ( History of Plato) in Hindi
- प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव( Influence of Socrates ) in Hindi
- प्लेटो की अवधारणा (Platonic Conception of Justice)- in Hindi
- प्लेटो (Plato): महत्त्वपूर्ण रचनाएँ तथा अध्ययन शैली और पद्धति in Hindi
- प्लेटो: समकालीन परिस्थितियाँ | (Contemporary Situations) in Hindi
- प्लेटो: आदर्श राज्य की विशेषताएँ (Features of Ideal State) in Hindi
- प्लेटो: न्याय का सिद्धान्त ( Theory of Justice )
- प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना | Criticism of Plato’s ideal state in Hindi
- प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, तथा क्षेत्र में योगदान
- प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन, गुण व दोष
- भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
- भारतीय संसद के कार्य (शक्तियाँ अथवा अधिकार)