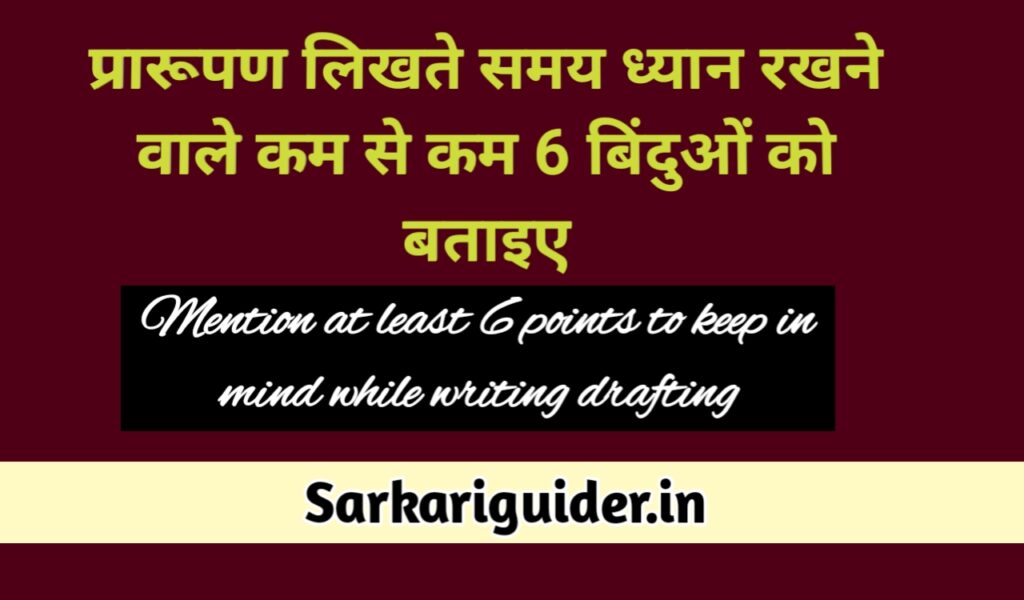
प्रारूपण लिखते समय ध्यान रखने वाले बिन्दु
प्रारूपण लिखते समय ध्यान रखने वाले बिन्दु- कार्यालयीय प्रारूपण की वैज्ञानिक और आदर्श प्रस्तुति के लिए हमें सबसे पहले आलेखन को रूपरेखा और उसके विभिन्न अवयवों पर गौर करना चाहिए। आलेखन की प्रस्तुत करते समय यदि हम इन अंगों पर क्रमबद्ध ध्यान नहीं देगे तो आलेखन की संरचना के अस्त व्यस्त और बेतरीन हो जाने का खतरा बना रहता है। इस दिशा में हमें पहले जिस विषय के सम्बन्ध में आलेखन प्रस्तुत करना है।, उसे विधिवत् समझ लेना चाहिए। इससे आलेखन तैयार करने में एक तो सुविधा होती है दूसरे, जिसके पास आलेखन प्रस्तुत करना होता है, उसे भी क्रमबद्ध पढ़ने में सुविधा होती है। बहरहाल, आलेखन के प्रमुख अंगों में सन्दर्भ या विषय का निर्देश, शीर्षनाम, प्रेषक और प्रेषिती के नाम तथा पदनाम, संख्या दिनांक संबोधन, विषय-वस्तु या प्रकरण से सम्बन्धित वक्तव्य, अनुच्छेद निष्कर्षात्मक परिच्छेद या समापन-मुख्य हैं। किसी भी श्रेष्ठ और उत्तम आलेखन की संरचना में इनका अनुपालन आवश्यक होता है। इन्हें क्रमशः निम्न प्रकार देखा जा सकता है-
1. कार्यालयीय आलेखन के विषय अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अलग-अलग स्वरूप के हो रहते हैं। अत: जिस तरह के मसौदे आलेखन यथा-बहुत गम्भीर या ह-के मामलों में सम्बन्धित होंगे उस तरह के अलग-अलग मसौदे तैयार किये जायेंगे इन मसौदों के निर्माण में तत्सम्बन्ध कार्यालय तथा वहाँ प्रयुक्त की जाने वाती शब्दावली का भी बड़ा सहयोग होता है साफ शब्दों में , शिक्षा विभाग के मसौदे और रेल विभाग या जीवन बीमा निगम के मसौदा की भाषा-शैली परस्पर भिन्न होगी।
2. अगली बात आलेखन की रूपरेखा निर्देश से सम्बन्ति होती हैं। जिस मसौदे को तैयार किया जा रहा है, यदि उसका सम्बन्ध पूर्व के किसी मामले या पत्र से है, तो उसका उल्लेख जिक्र या निर्देश कर देना चाहिए। इससे आलेखन प्राप्त करने वाले को पढ़ने में सुविधा होती है।
3. अगली बात आलेखन तैयार करने में शीर्षनाम का क्रम आता है। साफ शब्दों में जिस विभाग से प्रालेख निर्गत हो रहा है, उसका नाम आना चाहिए। कुल मिलाकर यह कि प्रारूप के ऊपर पत्र-प्रेषण कार्यालय का नाम, पता-प्रारूप संख्या तथा दिनांक लिखना चाहिए। इसके बाद प्रेषिती का नाम, पता एवं प्रारूप का मुख्य कलेवर उल्लिखित होता है। अन्त के प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है।
4. सामान्यतया विषय के बाद और कभी-कभार विषय के पूर्व संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह संबोधन प्रारूप के बायीं ओर लिखना चाहिए।
यह सम्बोधन सन्दर्भ के अनुसार जैसे- महोदय/महोदया, महानुभाव या प्रिय महोदय (अर्द्ध सरकारी पत्र की दिशा में) या प्रिय आदि में कुछ भी हो सकता है।
5. संबोधन के बाद मूल पत्र सामग्री या प्रकरण समाग्री या प्रकरण सम्बन्धी वक्तव्य दिया जाता है। यहाँ जिस पत्र का उत्तर दिया जा रहा है, उसका संदर्भ निर्देश या प्रस्तावना का उल्लेख करते हैं।
6. छोटे मसौदे में अनुच्छेद या उप विभाग की बहुत आवश्यकता तो नहीं होती, किन्तु यदि मसौदा दो-तीन पृष्ठों से ज्यादा का है तो प्रकरण या विषय-वस्तु ती समझ की सुविधा के लिए अनुच्छेदों का होना आवश्यक हो जाता है। हर संदर्भ यदि अलग अनुच्छेद में लिखा जाये तो और भी बढ़िया होगा, यथा अनुच्छेद संख्या 2, 3, 41 यह अनुच्छेद क्रमबद्ध होना चाहिए।
7. पत्र का निष्कर्षात्मक परिच्छेद या समापन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस समापन भाग में पूरे मसौद का निचोड़े आता है। यह मसौदा-पाठन में सहायक होता है। स्वनिर्देश के नीचे अधिकारीअपना हस्ताक्षर करता है। उस हस्ताक्षर के ठीक ऊपर हस्ताक्षर करने वाला स्त्री हो या पुरूष- भवदीय शब्द टाँकता है। यहाँ उसका पूरा नाम, उसका पदनाम तथा कार्यालय का पता लिखा होना बहुत आवश्यक होता है।
Important Links
- पारिवारिक या व्यवहारिक पत्र पर लेख | Articles on family and Practical Letter
- व्यावसायिक पत्र की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- व्यावसायिक पत्र के स्वरूप एंव इसके अंग | Forms of Business Letter and its Parts
- व्यावसायिक पत्र की विशेषताएँ | Features of Business Letter in Hindi
- व्यावसायिक पत्र-लेखन क्या हैं? व्यावसायिक पत्र के महत्त्व एवं उद्देश्य
- आधुनिककालीन हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ | हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल का परिचय
- रीतिकाल की समान्य प्रवृत्तियाँ | हिन्दी के रीतिबद्ध कवियों की काव्य प्रवृत्तियाँ
- कृष्ण काव्य धारा की विशेषतायें | कृष्ण काव्य धारा की सामान्य प्रवृत्तियाँ
- सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं | सगुण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
- सन्त काव्य की प्रमुख सामान्य प्रवृत्तियां/विशेषताएं
- आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ/आदिकाल की विशेषताएं
- राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ | रामकाव्य की प्रमुख विशेषताएँ
- सूफ़ी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ
- संतकाव्य धारा की विशेषताएँ | संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां
- भक्तिकाल की प्रमुख विशेषताएँ | स्वर्ण युग की विशेषताएँ
- आदिकाल की रचनाएँ एवं रचनाकार | आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ
- आदिकालीन साहित्य प्रवृत्तियाँ और उपलब्धियाँ
- हिंदी भाषा के विविध रूप – राष्ट्रभाषा और लोकभाषा में अन्तर
- हिन्दी के भाषा के विकास में अपभ्रंश के योगदान का वर्णन कीजिये।
- हिन्दी की मूल आकर भाषा का अर्थ
- Hindi Bhasha Aur Uska Vikas | हिन्दी भाषा के विकास पर संक्षिप्त लेख लिखिये।
- हिंदी भाषा एवं हिन्दी शब्द की उत्पत्ति, प्रयोग, उद्भव, उत्पत्ति, विकास, अर्थ,
- डॉ. जयभगवान गोयल का जीवन परिचय, रचनाएँ, साहित्यिक परिचय, तथा भाषा-शैली
- मलयज का जीवन परिचय, रचनाएँ, साहित्यिक परिचय, तथा भाषा-शैली
Disclaimer







Ji mujhe bahut achha laga ye apka topic but kuch short me likha kro plz
thanks …short ke liye try krenge