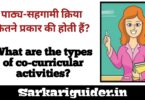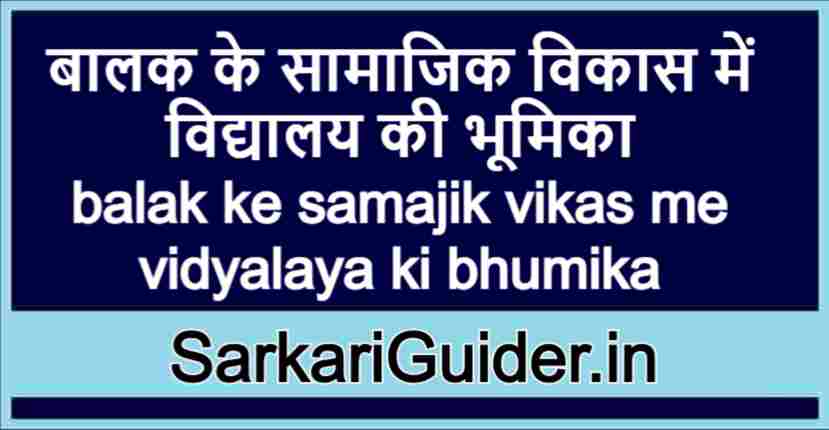
बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका
बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका की विवेचना से पूर्व विद्यालय के अर्थ को समझना आवश्यक है। विद्यालय का अर्थ निम्न परिभाषाओं से समझा जा सकता है-
ओटावे के अनुसार – “विद्यालय को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार समझना चाहिए जो समाज के बालकों के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण प्रदान करने के लिए हो।”
“The school may be regarded as a social invention to save society for the specialised teaching of younger ones. -A. K. C. Ottaway
जॉन डीवी के अनुसार-“विद्यालय का तात्पर्य एक ऐसे विशेष वातावरण से है जहाँ जीवन के कुछ गुणों एवं विशेष प्रकार की क्रियाओं एवं व्यवसायों की शिक्षा इस प्रयोजन से दी जाती है कि बालकों का वांछित दिशा में विकास हो।”
स्पष्ट है कि विद्यालय समाज द्वारा बनायी गयी संस्था है, अतः बालक के सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका को कम करके नहीं आँका जा सकता है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह समाज द्वारा मान्यता व्यवहार व कार्य बालकों को सिखाता है। विद्यालय की, बालकों के सामाजिक विकास में भूमिका की विवेचना निम्न बिन्दुओं के द्वारा की जा सकती है-
(i) विद्यालय बालकों की मानसिक क्रियाओं का विकास करता है, यथा-समझ, शक्ति; तर्क शक्ति, समस्या-समाधान आदि, जिससे बालक का सामाजिक विकास उन्नत चिन्तन होता है। बालक सही-गलत, उचित-अनुचित में भेद कर पाने में सक्षम हो पाते हैं।
(ii) विद्यालय समाज की सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों का संरक्षण करते हैं और नई पीढ़ी को हस्तान्तरित करते हैं।
(iii) समाज में सफल जीवनयापन के लिए आवश्यक है कि विद्यालय बालकों को प्रजातंत्र के लिए प्रशिक्षित करता है। बालक को उसके अधिकार और कर्त्तव्यों का ज्ञान देता है।
(iv) बालक को ज्ञान प्रदान करना ही विद्यालय का कार्य नहीं होता, बल्कि बालक को सामाजिक गुणों से सम्पृक्त करना भी विद्यालय का कार्य है।
(v) विद्यालय में अध्यापकगण और विद्यार्थियों के पारस्परिक सम्बन्ध, उनके द्वारा संचालित क्रियायें व विभिन्न कार्यक्रम, उनके आदर्श, सिद्धांत और मान्यतायें, अध्यापक और साथी टोली के सदस्यों का सामाजिक व्यवहार और गुण-दोष आदि सभी बातें बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं।
(vi) विद्यालय विविध प्रकार शैक्षिक प्रकरणों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालकों में सहयोग, सहकारिता, सत्यता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द्र, सहिष्णुता, त्याग जैसे गुणों का विकास करते हैं।
(vii) अपने धर्मनिरपेक्ष वातावरण से बालकों में धार्मिक और साम्प्रदायिक संकीर्णता पनपने से रोकते हैं।
(viii) विद्यालय में विविध पृष्ठभूमि के बालक आते हैं, साथ मिल-जुलकर विद्यालय की कक्षाओं में बैठते हैं, खाना खाते हैं, विविध कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस तरह उनका एक विद्यालयी समाज बन जाता है, जिससे अनुक्रिया करके उनकी समायोजन क्षमता विकसित होती है।
(ix) समाज के विभिन्न क्षेत्रों, आयामों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए इन्हें समझना आवश्यक होता है। विद्यालय बालकों को सामाजिक परिवर्तन का ज्ञान देते हैं।
विचारणीय बातें (Considerations) – बालक के सामाजिक विकास में अपनी प्रभावपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विद्यालयों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए-
(i) विद्यालय में आयोजित होने वाले क्रिया-कलाप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिए।
(ii) पाठ्यक्रमों को विविध संस्कृति के विविध आयामों से सम्पृक्त होना चाहिए।
(iii) विद्यालयों में ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियायें आयोजित की जानी चाहिए जिनसे बालकों को समान प्रशिक्षण प्राप्त हो सकें, जैसे- सामूहिक प्रार्थना, प्रातः सभा, पास-पड़ोस में समाज सेवा, श्रमदान, सफाई सप्ताह, विशेष उत्सवों पर सेवा आदि।
(iv) विद्यालयों को समूह कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे बालक सहकारिता के भाव सीख सकता है। वह दूसरों के साथ मिल-जुलकर कार्य करना सीखेगा।
(v) विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन भी अति महत्त्वपूर्ण होता है, इससे विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।
(vi) विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए, जिसमें ऐसी पुस्तकें, पत्रिकायें व पठन सामग्री होनी चाहिए जिससे बालक समाज के सफलतम महापुरुषों के गुणों और योग्यताओं से परिचित हो सकें।
(vii) विद्यालय में समय-समय पर प्रतिष्ठित समाज समर्पित व्यक्तियों का सम्भाषण आयोजित किया जाना चाहिए।
(viii) विद्यालय के कार्यक्रमों की आयोजन योजना बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये कार्यक्रम बालकों के सामाजिक विकास के लिए उपयोगी हों। उनमें अपने समाज की परम्पराओं, रीति-रिवाजों, मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न हो।
(ix) विद्यालयों को अपने कार्यक्रमों के संचालन में समुदाय के सदस्यों की प्रतिभागिता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। आदान-प्रदान की भावना के आधार पर विद्यालयों को अपनी योजनाओं और गतिविधियों को संचालित करना चाहिए। इससे विद्यालय और समाज एक-दूसरे के नजदीक आयेंगे और विद्यालयों द्वारा बालक के सामाजिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
(x) विद्यालयों को अपने कुछ कार्यक्रम विद्यालय की चहारदीवारी से बाहर भी आयोजित करने चाहिए। इससे बालकों का दृष्टिकोण विस्तृत होगा तथा वे अपने समाज की विरासत को समझ सकेंगे। पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में दौड़ रहे बालकों के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है।
(xi) बालक अनुकरण से बहुत कुछ सीखते हैं। बालक अध्यापकों का अनुकरण करते है। अध्यापक को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन समर्पण, प्रेम और सेवाभाव से करना चाहिए तभी वह स्वयं को उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। (xii) अध्यापकों को सचेत रहना चाहिए कि उसके विद्यार्थी अन्याय, हिंसा, अनैतिकता और मिथ्याचार जैसी बुराइयों से बर्बाद न हों।
(xiii) विद्यालयों में मार्गदर्शन सेवाओं (Guidance Services) की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। अक्सर बालकों को व्यावहारिक समस्याओं या साथी-समूह के दबाव से जूझना पड़ता है। ऐसे में बालकों की सहायता मार्गदर्शन द्वारा की जा सकती है।
(xiv) मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का ही सकारात्मक सामाजिक विकास सम्भव है। अध्यापक को बालक के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यदि उसे अहसास हो कि बालक तनाव, भग्नाशा, उदासी, कुण्ठा आदि का शिकार है तो उसकी सहायता करनी चाहिए।
Important Links
- सहभागिक अवलोकन का अर्थ और परिभाषा, विशेषतायें, लाभ अथवा गुण, कमियाँ अथवा सीमायें
- अवलोकन अथवा निरीक्षण की विधियाँ | नियन्त्रित और अनियन्त्रित अवलोकन में अंतर
- असहभागी अवलोकन- गुण, दोष | सहभागी व असहभागी निरीक्षण में अन्तर
- अवलोकन या निरीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएँ, उपयोगिता
- प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर | prashnavali aur anusuchi mein antar
- अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा, उद्देश्य, प्रकार, उपयोगिता या महत्व, दोष अथवा सीमाएँ
- प्रविधि का अर्थ | सामाजिक शोध की प्रविधियाँ
- साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा, विशेषताएँ, उद्देश्य, प्रकार, प्रक्रिया, तैयारी