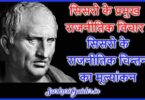सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या
सिद्धान्त : एक एकीकृत प्रक्रिया के रूप में
डायश का मत है कि राजनीतिक सिद्धान्तों को राजनीतिक ज्ञान और राजनीतिक कर्म के एक सृजनात्मकता चक्र के विभिन्न स्तरों के रूप में पहचाना जा सकता है। यदि उनमें से कोई भी स्तर उपेक्षित होता है तब सम्पूर्ण चक्र के टूटने की सम्भावना होती है, चक्र रूप भी करता है। किसी न किसी को इस क्षति की मरम्मत का उपाय ढूँढ़ना पड़ता है। स्मृतियों, अन्तर्दृष्टि व्यवस्थित प्रतीक चिन्ह, आत्मलोच, ह्यूरिस्टिक शोध कोई न कोई मूल्य लेकर चलती है, जिनके साथ प्रमाण योग्य-ज्ञान, प्रभुत्व सिद्ध क्षमता और जोखिम भरी बुद्धि हो सकती है। यह सब रजनीतिक सिद्धान्त के लिए जो राजनीतिक कर्म के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, स्वयं में आवश्यक है। राजनीतिक विचार और क्रिया भूतकाल में इन विभिन्न स्तरों में गुजरी है और भविष्य में गुजरती रहेगी।”
डायश का मत है कि इस दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धान्त अपनी समग्रता में एक एकीकृत व एकीकरण करने की प्रक्रिया है। यह आवश्यकता है कि उसकी एकता के लिए जागरूक प्रयास किये जाए। सिद्धान्त की एकता को एक बौद्धिक उद्यम के रूप में मानकर सुदृढ़ किया जाना चाहिए, चाहे उसमें राजनीतिक व्यवस्थाओं की विश्लेषणात्मक एकता विद्यमान हो अथवा नहीं।
सिद्धान्त निर्माण की प्रक्रिया
सिद्धान्त-निर्माण प्रक्रिया किसी बिन्दु, वस्तु, घटना, विचार प्रक्रिया, व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह, गतिविधियों आदि से प्रारम्भ होता है। सिद्धान्तीकरण से पूर्व कोई न कोई कारण अवश्य होता है। यह कारण या किसी व्यक्ति के विचार अथवा दृष्टिकोण से सम्बन्धित हो सकता है। अथवा अन्य किसी की माँग या प्रेरणा से हो सकता है। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति अथवा घटना के समस्त पक्षों से सम्बन्धित होकर उन्हें विशेष उद्देश्यों से सम्बन्धित पक्षों में ही देखता है। उदाहरण के लिए, एक राजनेता के व्यक्तित्व व जीवन के विविध पक्ष होते हैं। पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते समय उसके व्यक्तित्व के समस्त पक्षों से सम्बन्ध न रखकर केवल उसकी सार्वजनिक गतिविधियों से ही सम्बन्ध रखना पड़ता है। प्रयोजन से सम्बन्धित पक्ष ‘वस्तु, घटना अथवा व्यक्ति के पक्ष’ का आनुभविक अवलोकन करने पर उस प्रेक्षित भाग को तथ्य कहा जाता है। वस वस्तु अथवा व्यक्ति में विशेष रूप से पर्यवेक्षित किये गए गुणों के समुच्चय को अवधारणा, धारणा आदि कहा जाता है। अवधारणाओं का निर्माण कतिपय नियमों के आधार पर किया जाता है। अवधारणा से अध्ययनकर्त्ता यथार्थजगत् से अपने लिए तथ्यों का चयन करता है व इन तथ्यों को शब्दों अथवा प्रतीकों द्वारा सम्बन्धित करता है। इन शब्दों के कुछ गुणों अथवा विशेषताओं की ओर संकेत किया जाता है। वास्तव में अवधारणा शब्दों के द्वारा गुण समूहीकरण है। इस प्रकार के विविध समूहीकरण अपनी सामान्य विशेषताओं अथवा गुटों के आधार पर संवर्गों में बाँटे जा सकते हैं। अवधारणा में आने वाली वस्तुएँ अथवा घटनाएँ तथ्य कहलाती हैं। परिभाषाओं के द्वारा इन अवधारणाओं का स्वरूप निश्चित कर दिया है। परिभाषित अवधारणाओं को मापा जा सकता है। अवधारणाओं का प्रयोग अकेले नहीं होता वरन् उन्हें समुच्चय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न अवधारणाओं के मध्य समानताओं व असमानताओं का विश्लेषण कर उनका वर्गीकरण व्यापक अवधारणाओं के मध्य किया जाता है। यह वर्गीकरण कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। इस वर्गीकरण को संश्लेषणात्मक अथवा समन्वयात्मक अवधारणाओं द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह आवश्यक है कि वर्गीकरण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि यह परस्पर व्यापी न हो।
तदुपरान्त सिद्धान्त निर्माण का अलग चरण सामान्यीकरण आता है। सामान्यीकरण का अर्थ वस्तुओं, घटनाओं आदि के मध्य कुछ समानताओं व सामान्य रूप से पाई जाने वाली विशेषताओं का निर्णय सामान्यीकरण से अवधारणाओं के मध्य सम्बन्ध की अभिव्यक्ति होती है। सामान्यीकरण को प्राक्कल्पना नहीं माना जाना चाहिए। यह निश्चित, स्पष्ट व सशर्त होता है। मीहान के अनुसार सामान्यीकरण एक ऐसा प्रस्ताव अथवा सुझाव है जो घटनाओं के ही अथवा अधिक वर्गों को इस प्रकार सम्बद्ध करता है कि किसी एक संवर्ग में आने वाले सदस्य दूसरे प्रकार के वर्ग अथवा संवर्ग की भी सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। सामान्यीकरण भागमनात्मक अथवा निष्कर्षात्मक होते हैं। कभी-कभी वे उन बातों का भी वर्णन करते हैं जो देखी हुई नहीं होती।
तत्पश्चात् अन्तिम चरण स्वयं सिद्धान्त का निर्माण आता है। इस प्रक्रिया अथवा चरण में समान प्रकृति के सामान्यीकरण के मध्य सामस्य स्थापित किया जाता है। सिद्धान्त सामान्यीकरणों का एक ऐसा समुच्चय है जो सामान्य कथनों, विवरणों, अन्य सिद्धान्तों अथवा सामान्यीकरण की व्याख्या प्रस्तुत करता है।
राजनीति विज्ञान में पाये जाने वाले सिद्धान्त तीन वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं
(1) शाश्वत सिद्धान्त।
(2) सम्भावनात्मक सिद्धान्त ।
(3) प्रवृत्तिमूलक सिद्धान्त
सिद्धान्त-निर्माण के आयाम-सिद्धान्त निर्माण प्रक्रिया के चार आयाम हैं-
(1) प्रामाणिकता।
(2) जाँचशीलता।
(3) व्यापकता ।
(4) अवधारणात्मक रूपरेखा ।
प्रामाणिकता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक अवधारणा आनुभविक रूपसे पाये जाने वाले गुणों अथवा वलिशेषताओं के समूह से सम्बन्धित होनी चाहिए। जाँचशीलता से अभिप्राय है कि वह वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञातक की जाने वाली योग्य हो। उसमें बताए जाने वाले गुणों अथवा विशेषताओं की जाँच की जा सके। व्यापकता से अभिप्राय है कि व्यापकता से सिद्धान्त में अधिक वस्तुओं, घटनाओं आदि की विशेषताओं, सामान्य पारस्परिक सम्बन्धों आदि को व्यापक मात्रा में स्पष्ट किये जाने की विशेषता हो। जैसे-जैसे हम तथ्य से ऊपर की ओर सिद्धान्त व निर्माण की दशा में अग्रसर होते हैं, हम यह अनुभव करते हैं कि सिद्धान्त व अवधारणाओं की व्याख्यात्मकता में अभिवृद्धि होती जाती है। अवधाणात्मक रूपरेखा का उपयोग सिद्धान्त निर्माण अथवा विश्लेषण के लिए उपयुक्त घटनाओं, गतिविधियों तथा वस्तुओं आदि ‘तथ्यों’ के रूप में चयन के लिए किया जाता है।
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।