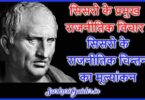राजनीति विज्ञान तथा राजनीतिक दर्शन में अन्तर
राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन में अन्तर का संकेत देने के लिए प्रायः यह कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान का सरोकार यथार्थ या तथ्यों से है, जबकि राजनीतिक दर्शन का सरोकार आदर्श, मानको और मूल्यों से है। दूसरे शब्दों में, राजनीति विज्ञान यह पता चलता है कि मनुष्य राजनीतिक स्थिति में क्या-क्या करते हैं; राजनीतिक दर्शन पर यह निर्धारित करता है कि ऐसी स्थिति में मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने न्याय को सद्जीवन का सर्वोपरि सिद्धान्त मानते हुए इसकी सिद्धि के लिए के लिए आदर्श राज्य व्यवस्था का निरूपण किया।
इस दृष्टि से विचार किया जाए तो राजनीतिक दर्शन, राजनीति विज्ञान का आधार दिखाई देता है।
इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत हम शुभ और अशुभ, उचित और अनुचित के बारे में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए वस्तुस्थिति की समालोचना करते हैं, और फिर यथार्थ को आदर्श के अनुरूप ढालने के लिए नई व्यवस्था के निर्माण का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इस तरह राजनीतिक दर्शन का सरोकार ‘तथ्यों’ और ‘मूल्यों’ दोनों से है। परन्तु इन दोनों का एक साथ निर्वाह सचमुच कठिन कार्य है। मुख्य समस्या वहाँ पैदा होती है जहाँ कोई दार्शनिक तथ्यों और मूल्यों को आपस में मिलाकर व्याख्या और वकालत में अन्तर करना भूल जाता जो एक स्वाभाविक मूल है। इसका कारण परम्परागत राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा वास्तविक तथ्यों को और जो सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों की परिवर्तन गति में स्वाभाविक रूप से पैदा होते हैं। परम्परागत राजनीतिक दार्शनिक तथ्यों के अन्वेषण के लिए उतने सजग नहीं रह पाते, जितनी आज की राजनीति विज्ञान के अन्तर्गत माँग की जाती है। पुराने दार्शनिकों के पास तथ्यों के निरीक्षण के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं थे, और वे आधुनिक सांख्यिकीय तकनीकों से भी परिचित नहीं थे। उनकी कृतियों में तथ्यों के विवरण के साथ-साथ अनेक काल्पनिक बातें भी आ गयी हैं। उदाहरण के लिए, निकोलो मैकियावली (1469-1527), टामस हाब्स (1588-1679) और जॉन लॉक (1632-1704) ने अपने-अपने सीमित अनुभव के आधार पर मानव प्रकृति के बारे में अपनी-अपनी मान्यताएँ प्रस्तुत की हैं। इसमें ‘सच-मुच पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना ‘अच्छे-बुरे’ पर दिया गया है। ऐसी मान्यताओं को विज्ञान की कसौटी पर नहीं परखा जा सकता। अतः आधुनिक मनोविज्ञान के अन्तर्गत मानव प्रकृति का अन्वेषण करते समय इन मान्यताओं की जाँच नहीं की जाती। फिर हॉब्स और लॉक के नागरिक समाज के संगठन के पूर्व जिस प्राकृतिक दशा का विवरण दिया है, यह सर्वथा काल्पनिक है, और इसलिए ये दोनों विवरण एक दूसरे से इतने भिन्न हैं। दूसरी ओर, जब हम आधुनिक सामाजिक मानव-विज्ञान के अन्तर्गत प्रमाणों के आधार पर नागरिक समाज की स्थापना से पहले के सामाजिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें ऐसे अन्तर्विरोधों की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसी हॉब्स और लॉक के विवरणों में पाई जाती है। वैज्ञानिक ज्ञान के अन्तर्गत कोई भी व्याख्या निरीक्षण और प्रमाण के आधार पर दी जाती है। यहाँ जब किसी घटना की कोई व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है, तब पुरानी व्याख्याएँ त्याग दी जाती हैं, परन्तु राजनीतिक दर्शन के अन्तर्गत अनेक व्याख्याएँ एक साथ प्रचलित रह सकती हैं।
इसका एक प्रधान कारण यह है कि राजनीतिक दर्शन जिन स्थितियों की व्याख्या करना चाहता है, वे मानवीय जीवन की आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों से सम्बन्ध रखती हैं। वैधानिक सिद्धान्त से न तो इनका पता लगा सकते हैं, न इनकी जाँच ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति और राज्य के परस्पर सम्बन्ध पर विचार करते हुए थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ज्यां जाग रूसो (1712-1778), जी. डब्ल्लू. एफ. हीगल (1770-1831), टी. एच. ग्रीन. (1836-1882) और एच.जे. लॉस्की (1893-1950) ने अपनी-अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने-अपने ढंग से राजनीति का दायित्व के भिन्न-भिन्न आधार और भिन्न-भिन्न सीमाओं का विवरण दिया है। इनमें से कौन-कौन सी मान्यताएं कितनी युक्ति युक्त हैं- इस पर तर्क-वितर्क हो सकता है, परन्तु कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। इसी तरह, लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धान्त रखा, उसका कोई अनुभवमूलक आधार नहीं ढूंढा जा सकता। निःसन्देह यह तर्क हमें प्रत्यक्ष रूप में उचित प्रतीत होता है। क्योंकि जिन राजनीतिक विज्ञानियों की वैज्ञानिक दृष्टि केवल तथ्यों से ही वैज्ञानिक आधार माना जाता है, वह उन्हीं में विज्ञान का आधार देखते हैं तथा राजनीति दर्शन की परम्परा से हमें तथ्यों के बारे में सर्वथा प्रमाणिक जानकारी चाहे न भी मिले, परन्तु मानव-जीवन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने में इससे सहायता अवश्य मिलती है। जैसे प्रत्येक पीढ़ी को नया वाहन बनाने से पहले पहिए का आविष्कार नहीं करना पड़ता, वैसे ही हमें अपना राजनीतिक तर्क प्रस्तुत करने के लिए नई संकल्पनाओं और ई शब्दावली का निर्माण नहीं करना पढ़ता। हम अपनी आधुनिक चेतना के आलोक में ही युग-युगान्तर से प्रचलित तर्क श्रृंखला को परख कर उपर्युक्त दृष्टिकोण बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अरस्तू ने दास प्रथा का समर्थन करते हुए यह तर्क दिया था कि केवल स्वतन्त्रजन ही सद्गुण की क्षमता रखते है, दास में यह क्षमता नहीं पाई जाती; अतः दास का जीवन स्वामी की सेवा में सार्थक होता है। आज के युग में दास-प्रथा तो प्रचलित नहीं है, परन्तु सामाजिक विषमता की ज्वलंत समस्या अवश्य विद्यमान है। रूसो ने प्राकृतिक विषमता और परम्परागत विषमता में जो अन्तर स्पष्ट किया था, उससे इस विषमता के विश्लेषण का तर्कसंगत मानदंड प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु इस विषमता के कई समर्थक अरस्तू के तर्क को ही घुमा घुमा कर दोहराते दिखाई देते हैं। कुछ समय पहले तक उपनिवेशवाद के समर्थक भी कुछ ऐसा ही तर्क देते थे। ऐसे किसी भी सिद्धान्त को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले अरस्तू के तर्क को परखना जरूरी हो जाता है। हम देखते हैं कि ‘सद्गुण की क्षमता’ के बारे में अरस्तू की सारी धारणा गोलमोल है; मानवीय क्षमताओं की तुलना इस आधार पर नहीं हो सकती। इनकी तुलना शारीरिक शक्ति, बुद्धि-लब्धि और अभिक्षमता-परीक्षण, इत्यादि के आधार पर की जा सकती है और इनमें भारी अन्तर नहीं पाये जाते कि एक स्तर के लोगों को स्वामी बनने योग्य समझा जाए, और दूसरे स्तर के लोगों को दास बनने योग्य माना जाए। इस मामले में जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट (1724-1804) का दृष्टिकोण आधुनिक चेतना के अनुरूप है। इनके अनुसार, प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य के नाते गरिमा से सम्पन्न होता है कि जिसे किसी सांसारिक मूल्य से नहीं तोला जा सकता। अतः प्रकृति ने किसी को किसी का दास नहीं बनाया। प्रत्येक मनुष्य अपने-आप में साध्य है; कोई मनुष दूसरे के साध्य का साधन नहीं हो सकता। सब मनुष्य प्रकृति से स्वतन्त्र हैं और वे अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही परस्पर लाभ के लिए एक दूसरे के प्रति कोई दायित्व स्वीकार करते हैं, शर्त यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने-आप में साध्य रहेगा। कोई भी मनुष्य किसी भी हालत में ऐसा दायित्व स्वीकार नहीं कर सकता कि वह अपनी स्वतन्त्रता का त्याग करके दूसरे की सम्पत्ति बन जाएगा। यह बात महत्त्वपूर्ण है कि समकालीन राजनीति-दार्शनिक जॉन राल्स ने मनुष्यों के बारे में ऐसी संकल्पना के आधार पर ‘न्याय’ का विस्तृत सिद्धान्त विकसित किया है।
कुछ आलोचक यह तर्क देते हैं कि पुराने राजनीति चिन्तन जिन-जिन परिस्थितियों में प्रस्तुत किया गया, वे अब अदल चुकी हैं, अतः आज के युग में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई हैं। यह तर्क बहुत युक्तियुक्त है। माना की पुराने राजनीति दर्शन का मुख्य सरोकार अपने-अपने समय की राजनीति से था, परन्तु उसके अन्तर्गत मनुष्य और समाज के बारे में चिरंजन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है। उसमें ऐसी समस्याएँ उठाई गई हैं जो देश-काल की सीमाओं से परे हैं—जो देश-देशान्तर और युग-युगान्तर के लिए पर्याप्त प्रासंगिक हैं। ऐसा चिन्तन ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज तो है, परन्तु वह सार्वजनीन और सर्वकालीन चर्चा का विषय है। किसी भी विचारक के चिन्तन का कुछ अंश उसकी परिस्थितियों और प्रयोजनों की अभिव्यक्ति हो सकता है; उसका विश्लेषण करके हम उसके सार्वजनीन और सर्वकालीन अंश की पहचान कर सकते हैं, और इसके आधार पर अपने राजनीतिक तर्क का निर्माण कर सकते हैं। यह नहीं मान लेना चाहिए कि पुराना सारा चिन्तन किन्हीं विशेष परिस्थितियों और प्रयोजनों का परिणाम मात्र है। उदाहरण के लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य को जो संकल्पना प्रस्तुत की, उसे हम कल्पना लोक का चित्र मान कर अस्वीकार कर सकते है, परन्तु उसने लोकतन्त्र के अन्तर्गत राजनीतिज्ञों की चालबाजियों का जो विवरण दिया है, वह आज भी पूर्णतः सही मालूम होता है। अरस्तु ने दास प्रथा के पक्ष में जो तर्क दिए, उन्हें चाहे हम स्वयं को स्वम्य या मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील होने की आड़ में स्वीकार न करें, परन्तु उसने राज्यों के अन्तर्गत विद्रोह के जो कारण स्पष्ट किए, वे आज भी सार्थक प्रतीत होते हैं। मैकियावली ने राजनीति और नैतिकता के बीच जो दीवार खड़ी की, उसे हम मान्यता नहीं। देते, परन्तु कूटनीति के क्षेत्र में हम उसकी अनोखी सूझ-बूझ से लाभ उठा सकते हैं। हॉब्स ने मानव-प्रकृति का जो विवरण दिए हैं, उसे हम ज्यों-के-ज्यों स्वीकार नहीं कर सकते, परन्तु उसे हम बुर्जुआ मानव के व्यवहार का दर्पण मानकर पूँजीवाद के विश्लेषण के लिए अन्तर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जिसमें मनुष्य सभ्य समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने स्वार्थ-साधन के प्रति निरन्तर सजग और सचेत रहता है। आज हम यह पालन करते हुए अपने स्वार्थ-साधन के प्रति निरन्तर सजग और सचेत रहता है। आज हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि हॉब्स कानून और व्यवस्थापरक राज्य (का प्रवक्ता है, कल्याणकारी राज्य या ‘सेवाधर्मी राज्य’ की संकल्पना के लिए उसके चिन्तन में कोई गुजाइश नहीं है। लॉक के चिन्तन में हमें सम्पत्ति के अधिकार के दार्शनिक आधार का विवरण देखने को मिलता है जो उदीयमान पूँजीवादी व्यवस्था को सहारा देने के लिए जरूरी था। आज हम लॉक की तरह सम्पत्ति के अधिकार को परम पावन तो नहीं मानते, परन्तु उसने सरकार को एक ‘न्यास’ या ट्रस्ट के रूप में में स्थापित करके संविधानवाद का जो आधार प्रस्तुत किया, उसे हम आज भी महत्त्वपूर्ण समझते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धान्त में हमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सर्वोत्तम संकेत मिलता है जो कि आधुनिक लोकतंत्र की बुनियाद है। हीगल के चिन्तन में हमें नागरिक समाज के अन्तर्गत राजनीतिक दायित्व का आधार मिलता है, वह आज भी सार्थक हैं, हालांकि उसने राष्ट्र-राज्य का जो गौरव-गान किया है, उसे हम ज्यों-के-त्यों स्वीकार नहीं कर सकते। कार्ल मार्क्स (1818-1883) की आरम्भिक कृति ‘इकॉनॉमिक एंड फिलॉसफिक मैनुस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844’ (1844) की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ) के अन्तर्गत बुर्जुआ समाज की जो आलोचना प्रस्तुत की गई थी। उसे समकालीन सन्दर्भ में हबर्ट मार्क्यूजे (1898 1979) के नए रूप में विकसित किया है। अरस्तू ने लोकतंत्र की परिभाषा ‘निर्धन बहुमत के शासन के रूप में देकर उसकी त्रुटियों की ओर संकेत किया था। समकालीन सन्दर्भ में सी.बी. मैक्फर्सन (1911-1987) में लोकतंत्र की सार्थकता के लिए उसकी यही परिभाषा फिर से अपनाने का समर्थन किया। हालांकि निर्धन वर्ग को सार्वजनिक नीति के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाने की शक्ति प्रदान की जा सके। समकालीन राजनीति दार्शनिक जॉन राल्स ने न्याय सिद्धान्त के अन्वेषण के लिए लॉक की अनुबंधमूलक सिद्धान्त को नए रूप में अपनाने का प्रयत्न किया है, और विवेकशील वार्ताकारों की संकल्पना के लिए मनुष्य के बारे में कांट की कल्पना को अपनाया है। इसी तर्क शैली के आधार पर राल्स ने जरमी बेंथम (1748-1832) और जे. एस. मिल (1806 1873) के उपयोगितावाद तीखा प्रहार किया है। न्याय सिद्धान्त के दूसरे समकालीन व्याख्याकार रॉबर्ट नॉजिक ने लॉक की ही अनुबंधमूलक पद्धति का सहारा लेकर स्वेच्छातंत्रवाद की पुष्टि की है। जो राल्स के समतावाद से सर्वथा भिन्न है। दूसरी ओर, स्वेच्छातंत्रवाद के समकालीन प्रवर्तक मिल्टन फ्रीडमैन ने हर्बर्ट स्पेंसर की अस्सी साल पुरानी तर्क शैली को नए रूप में दोहराने का प्रयत्न किया है। इस तरह राजनीति दर्शन में जिन संकल्पनाओं का प्रयोग होता है, वे निरन्तर चर्चा-परिचर्चा का विषय बनी रहती हैं और नए चिन्तन के लिए आधार का काम देती हैं।
इसे भी पढ़े…
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।