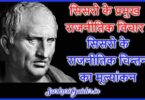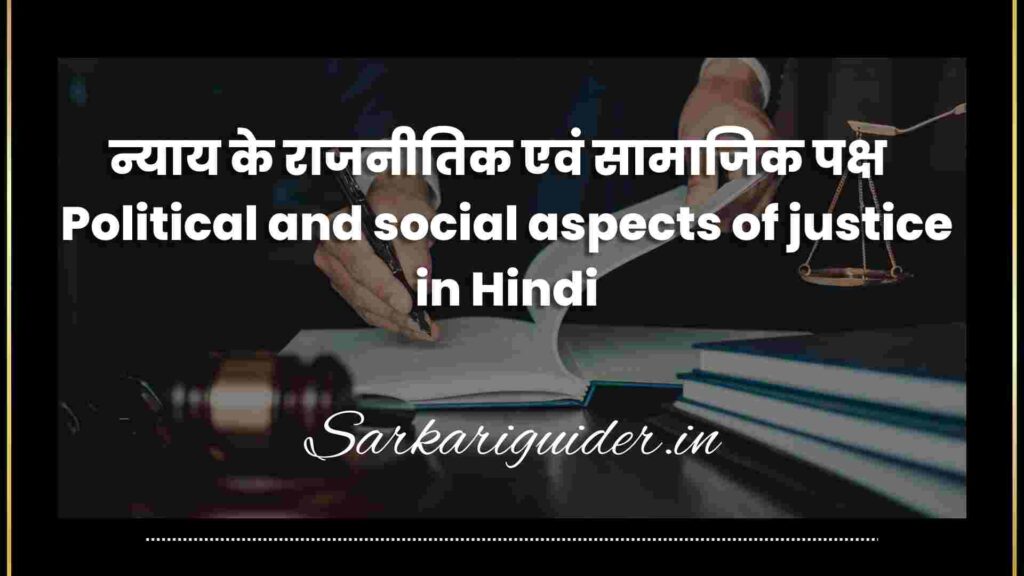
न्याय के राजनीतिक एवं सामाजिक पक्ष | Political and social aspects of justice in Hindi
(1) न्याय का राजनीतिक पक्ष- मानव अधिकार घोषणा-पत्र (Universal Declaration of Human Rights) का 20वां अनुच्छेद कहता है कि “प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की शासन व्यवस्था में हाथ बँटाने का अधिकार है।” दूसरे शब्दों में, राजनीतिक दृष्टि से कोई “अभिजात या विशेषाधिकार प्राप्त-वर्ग” नहीं होगा। सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे। राजनीतिक न्याय के महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं-
(i) मताधिकार (Right to Vote)- फ्रांस के क्रांतिकारियों की एक मुख्य माँग यह थी कि धन व कुल के भेदभाव के बिना सभी को राजनीतिक अधिकार प्रदान किये जायें। केवल धन के आधार पर ही मताधिकार का प्रयोग निश्चय ही एक अन्यापूर्ण व्यवस्था मानी जायेगी। इसका कारण यह है कि मात्र धनी होना ही इस बात की गारण्टी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का सही-सही उपयोग कर सकेगा। आधुनिक युग में ‘वयस्क मताधिकार’ (Adult Franchies) के सिद्धान्त को ही न्यायपूर्ण माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक बालिग व्यक्ति को, यदि वह पागल नहीं है, मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस मान्यता के तीन प्रमुख कारण निम्न हैं-
प्रथम, लोकतन्त्र तब तक ‘वास्तविक लोकतन्त्र’ नहीं हो सकता जब तक कि प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्येक नागरिक का योगदान न हो। प्रत्येक व्यक्ति इतनी क्षमता अवश्य रखता है कि वह मत देने के अधिकार का समझदारी के साथ उपयोग कर सके।
द्वितीय, मताधिकार से सामान्य लोगों के मन में गौरव व स्वाभिमान का भाव जाग्रत होता है। उन्हें लगता है कि वे शासन-तन्त्र से कटे हुए नहीं हैं बल्कि शासन-संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
तृतीय, मताधिकार नागरिकों के अन्य अधिकारों को सुरक्षित रखने का साधन है। वह शासनाधिकारियों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। मताधिकार से लोगों को अपनी वास्तविक शक्ति का बोध होता है। हम मतदान का प्रयोग करके ऐसी सरकार को बदल सकते हैं जो हमारी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती फलस्वरूप, हिंसक क्रांति की सम्भावना नहीं रहती। मैकरिडिस और वार्ड (Macridis & Ward) के शब्दों में, “जिन देशों में यत्नपूर्वक समाज के किन्हीं विशिष्ट वर्गों को राजनीतिक सत्ता से वंचित रखा जाता है, वहाँ ये वर्ग हिंसक साधनों से सत्ता हथियाने का प्रयास करते हैं।”
(ii) अन्य अधिकार व स्वतन्त्रताएँ (Other Rights and Liberties) – मताधिकार के अतिरिक्त जिन अन्य अधिकारों व स्वतन्त्रताओं को आवश्यक समझा गया है, उनमें मुख्य मुख्य ये हैं— नागरिकों को चुनावों में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए, सरकारी पदों पर नियुक्ति की सभी को समान सुविधाएँ प्राप्त हों तथा विचारों की अभिव्यक्ति व राजनीतिक दलों का गठन करने की सभी को स्वतन्त्रता हो।
(iii) मानव अधिकारों की सावधानी से रक्षा (Sufficient Attention to Human Rights ) – मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतन्त्रताओं के प्रति सम्मान की भावना बहुत आवश्यक है। न्यूयार्क स्थित ‘फ्रीडम हाउस’ की एक रिपोर्ट के अनुसार आज भी विश्व के दो-तिहाई से अधिक देशों में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। कम्युनिस्ट देशों में राज्य का शिकंजा अब उतना कठोर नहीं है जितना कि 20-30 वर्ष पहले था, फिर भी इन देसों में मानव अधिकारों का हनन एक सामान्य बात है। रूस और चीन में शासन-विरोधियों पर होने वाले अत्याचारों के समाचार समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। बर्मा (म्यांमार), पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में हजारों नागरिकों को अकारण जेल में रखा जा चुका है। इण्टरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (International Press Institute )– ने सन् 1984 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह बात कही थी कि “विभिन्न देशों की सरकारों ने अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन किया है तथा संचार माध्यमों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाये हैं।”
( 2 ) न्याय का सामाजिक पक्ष (Social Dimension of Justice )- न्याय का एक सामाजिक पक्ष भी है। सामाजिक जीवन अनेक विविधाओं से पूर्ण है। समाज में परिवार है, चर्च है, संघ है, विभिन्न सांस्कृतिक व व्यावसायिक समुदाय हैं तथा विविध सम्प्रदाय और धर्मों के मानने वाले लोग हैं। भारत जैसे देश में तो जातिभेद भी है और हरिजन तथा गैर-हरिजन की समस्या भी है। इसके अतिरिक्त हिन्दुओं और मुसलमानों के कुछ निजी कानून हैं जिन्हें लागू करना अदालतों का कर्त्तव्य है। ऐसी स्थिति में सामाजिक न्याय का प्रश्न अत्यधिक जटिल बन गया है। इस सम्बन्ध में कुछ विचारणीय बातें निम्नलिखित हैं-
(i) सामाजिक व धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप ( State’s Intervention in Socio-religious Affairs ) – इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि धार्मिक परम्पराओं और सामाजिक रीति-रिवाजों में राज्य किस सीमा तक हस्तक्षेप कर सकता है? मैकडाइवर का कथन है कि धार्मिक विश्वास और आन्तरिक नैतिकता से सम्बन्धित मामले राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त रहने चाहिए। कला, साहित्य, संगीत, फैशन और रीति-रिवाजों के क्षेत्र में भी नागरिक स्वतन्त्र हैं। इसी प्रकार पारिवारिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। न्याय का क्योंकि स्वतन्त्रता से सम्बन्ध है, इसलिए इन क्षेत्रों में राज्य का अनुचित हस्तक्षेप निश्चय ही न्याय संगत नहीं माना जा सकता किन्तु प्रश्न यह है कि उचित और अनुचित के बीच विभाजक रेखा कैसे खींची जाये ? सार्वजनिक शान्ति और व्यवस्था (Public Order), सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Property) और सार्वजनिक सदाचार (Public Morality) की रक्षा के लिए तो राज्य को कानून बनाने ही पड़ेंगे।
(ii) कुछ बातों के आधार पर भेदभाव से इन्कार (Probhibition of Discriminiation)-निस्संदेह न्याय का तकाजा है कि नागरिकों के साथ केवल रंग, वंश या जाति के आधार पर कोई पक्षपात न किया जाये किन्तु प्रश्न यह है कि पक्षपात न किये जाने की बात केवल सार्वजनिक कर्तव्यों के सम्बन्ध में ही उचित है या निजी मामलों में भी वह उतनी ही उचित है? यह तो माना जा सकता है कि एक ‘श्वेत’ व्यक्ति जो कि सार्वजनिक पद पर आसीन है कोई भी निर्णय लेते समय या नियुक्ति करते समय काले-गोरे का भेदभाव न रखे किन्तु क्या उसे इस बात के लिये भी विवश किया जा सकता है कि वह अपना मकान नीग्रो को ही किराये पर उठाये ? यह एक पेचीदा प्रश्न है। सामान्यतः निजी मामलों में लोगों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए किन्तु यदि स्वतन्त्रता से समाज के एक बड़े वर्ग को कष्ट पहुँचता हो तो राज्य अवश्य हस्तक्षेप करेगा। अब सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि जहाँ तक सार्वजनिक भोजनालयों, दुकानों, शिक्षणालयों, मनोरंजन के स्थानों, तलाबों, कुओं आदि का प्रश्न है, उनके प्रयोग से कोई भी व्यक्ति केवल धर्म, वंश, जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।
(iii) शोषण का निषेध (Prohibition of Exploitation )- सामाजिक न्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मानव का मानव द्वारा शोषण समाप्त किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान ने न्याय के इस आदर्श की पुष्टि की है। संविधान द्वारा मानव-व्यापार तथा किसी व्यक्ति से बेगार अथवा जबर्दस्ती काम लेना गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया है।
अनेक लेखकों व विचारकों का मत है कि कानून द्वारा शोषण पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बाद भी भारत का पिछड़ा वर्ग अपने को सुरक्षित अनुभव नहीं कर रहा है। इसका कारण यह है कि इन लोगों की समस्या जाति-भेद से उत्पन्न होते हुए भी मूलतः आर्थिक है।
(iv) काम की यथोचित् व मानवोचित दशाएँ (Just and Human Conditions of Work ) – यह आवश्यक है कि राज्य काम की मानवोचित दशाएँ सुनिश्चित करे। दूसरे शब्दों में, सभी को सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के अवसर प्राप्त होने चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य का स्तर ऊँचा किया जाना चाहिए तथा नागरिकों की शैक्षिक उन्नति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
इसे भी पढ़े…
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।
- सिख धर्म की प्रमुख विशेषताएं | Characteristics of Sikhism in Hindi
- भारतीय समाज में धर्म एवं लौकिकता का वर्णन कीजिए।
- हिन्दू धर्म एवं हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त
- भारत में इस्लाम धर्म का उल्लेख कीजिए एवं इस्लाम धर्म की विशेषताएँ को स्पष्ट कीजिए।
- इसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म की विशेषताएं
- धर्म की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए।
- मानवाधिकार की परिभाषा | मानव अधिकारों की उत्पत्ति एवं विकास
- मानवाधिकार के विभिन्न सिद्धान्त | Principles of Human Rights in Hindi
- मानवाधिकार का वर्गीकरण की विवेचना कीजिये।