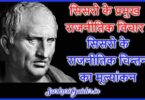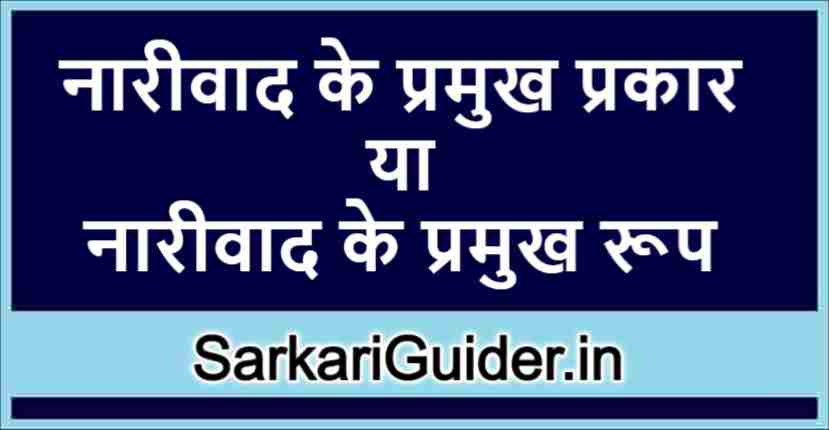
नारीवाद के प्रमुख प्रकार या रूप
नारीवाद गत लगभग तीन सदियों में तीन सैद्धान्तिक प्रस्थापनाओं के रूप में सामने आया तथा इन्हें ही नारीवद के प्रमुख प्रकार कहा जा सकता है :
1. उदारवाद नारीवाद
उदारवाद नारीवाद लिंग समानता में विश्वास करता है और एक सेक्स द्वारा सेक्स को अपने अधीन करने या नारी को समान स्तर का मानव प्राणी न समझते हुए, उसे ‘काम सम्बन्धों’ (सेक्स रिलेशन्स) का एक साधन मात्र मानने की धारणा का विरोध करता है। उदारवाद नारीवाद के अनुसार, नारी का मुख्य कर्यक्षेत्र तो घर है लेकिन इच्छा, आवश्यकता और परिस्थितियों से प्रेरित होकर यदि स्त्री घर के बाहर कोई भूमिका निभाती है तो परिवार, समाज और समस्त व्यवस्था द्वारा इस स्थिति को पूरे मन से स्वीकार किया जाना चाहिए। नारीवाद का यह रूप पुरुष को धिक्कारता नहीं, पुरुष को समानता के आधार पर स्वीकार करता है। मूल बात यह है स्त्री और पुरुष, कि नारी के व्यक्तित्व को सभी प्रकार से पुरुष व्यक्तित्व के समान, किसी भी रूप में पुरुष व्यक्तित्व से कम महत्वपूर्ण नहीं, समझा जाना चाहिए। जे.एस. मिल की प्रसिद्ध पंक्ति है, ‘अपने ऊपर, अपने शरीर मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति सम्प्रभु है’ मिल की यह बात, दोनों पर समान रूप से और सामान सीमा तक लागू होती है।
2. मार्क्सवादी नारीवाद
मार्क्सवाद के अनुसार, नारी के शोषण के दो कारणा हैं प्रथम कारण है, पैतृक सत्ता (पुरुष की सत्ता पर आधारित परिवार और समाज व्यवस्था) द्वितीय, निजी सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व की इस व्यवस्था के कारण नारी के श्रम (बच्चों का पालन-पोषण और परिवारिक कार्य ) का उपयोग मूल्य’ तो है, ‘विनिमय मूल्य’ नहीं है। स्त्री के कार्य का मुद्रा के रूप में कोई भुगतान नहीं होता तथा इस बात ने स्त्री को पुरुष के अधीन बना दिया है। मार्क्सवादी नारीवाद पूंजीवादी व्यवस्था और पैतृकता को परम्पर निर्भर व्यवस्थाएं मानता है, जिल्ला आइजेनटीन इसे ‘पूंजीवादी पैतृकता’ मानते हैं। मार्क्सवादी नारीवाद इस बात पर बल देता है कि नारी की मुक्ति के लिए दो दिशाओं में एक साथ कार्य करना होगा, क्योंकि ये दोनों तत्व नारी शोषण के लिए एक-दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। पुरुष की सत्ता का अन्त कर समानता पर आधारित समाज व्यवस्था को अपनाना होगा तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की व्यवस्था का अन्त करना होगा। आर्थिक व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन के बिना, नारी मुक्ति मात्र एक दिवा स्वप्न बनी रहेगी ।
3. रेडीकल फेमीनिज्म या उग्रवादी नारीवाद
नारीवाद का यह सर्वाधिक आक्रोशपूर्ण एवं उग्रवादी रूप है। उग्रवादी नारीवाद ने यह प्रतिपादित किया कि नारियों की दयनीय स्थिति का मूल कारण पुरुष की प्रभुता वाला समाज है। यह पुरुष प्रधान समाज अपने को विवाह और परिवार संस्था के माध्यम से सम्पोषित करता रहा है। इस प्रकार पैतृक समाज की जड़ें समाज के आर्थिक कारकों में नहीं, वरन् जीवन विज्ञान में हैं। महिला की प्रजनन क्षमता इसका आधार है।
महिलाओं की मुक्ति तभी सम्भव है, जब ‘जैविक परिवार’ की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए अर्थात् यह सामाजिक संगठन का आधार न रहे। विवाह के आधार पर बच्चों के जन्म और परिवार में बच्चों के पालन-पोषण के स्थान पर उग्रवादी नारीवाद ‘स्वतन्त्र सेक्स और बच्चों की सामूहिक देखभाल’ की वकालत करता है। यह मार्ग ही मातृक सत्ता को जन्म देगी।
रेडीकल फेमीनिज्म ‘आक्रोशपूर्ण मात्र सैद्धान्तिक अतिरंजना’ मात्र है तथा सैद्धान्तिक दृष्टि से भी नारीवादियों के एक छोटे समूह की मानसिक उपज है, नारीवादियों ने व्यापक रूप से या सामान्य रूप से इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया। नारीवाद के नाम पर सदियों से जांची-परखी संस्था परिवार को समाप्त करने की बात का कोई औचित्य नहीं है। परिवार का अन्त नारी मुक्ति का मार्ग नहीं है। ‘फ्री सेक्स’ की स्थिति नारी मुक्ति को नहीं, वरन् घोर अव्यवस्था और ‘शक्ति ही सत्य है’ की स्थिति को ही जन्म देगी।
इसी प्रकार मार्क्सवादी नारीवाद की इस बात को भी स्वीकार कर पाना सम्भव नहीं है कि “पैतृक समाज और पूंजीवादी व्यवस्था परस्पर निर्भर स्थितियां या व्यवस्थाएं हैं। नारी मुक्ति और मार्क्सवादी समाज में कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित कर पाना सम्भव नहीं है। अतः नारीवाद के इन तीन रूपों में उदारवादी नारीवाद को ही नारीवाद की सामान्य रूप से स्वीकृत स्थिति समझा जा सकता है लेकिन उदारवादी नारीवाद की धारणा को समय के साथ आगे बढ़ना होगा। नारी व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता, नारी एकता और नारी सशक्तिकरण को ही अधिक अंशों, में, बहुत अधिक अंशों में अपनाना होगा।
इसे भी पढ़े…
- राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की परिभाषा | राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व
- एक राजनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के गुण और दोष
- एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त की सत्यता का विवेचन कीजिए।
- अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए।
- अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।