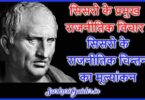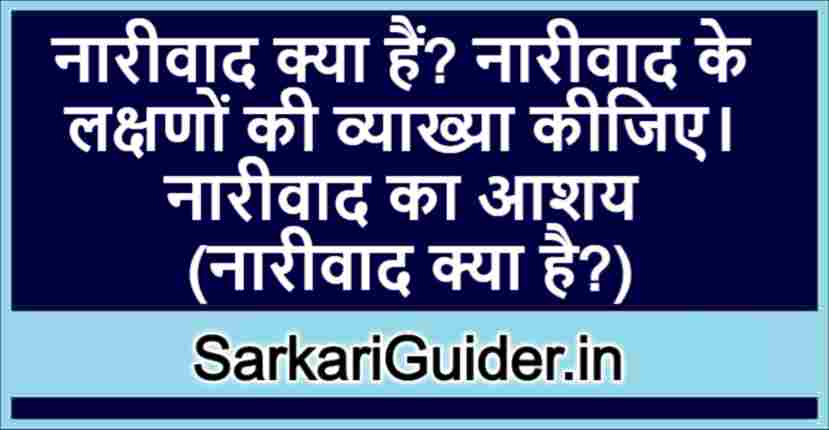
नारीवाद क्या हैं?
नारीवाद सामान्यता वह विचारधारा और आन्दोलन है जिसका उद्देश्य है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त हो। परम्परागत रूप से और समकालीन जीवन में भी महिलाओं को अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति ही प्राप्त है। नारीवाद का लक्ष्य है इस अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति को समाप्त कर उन्हें परिवार, समाज, राज्य और समूचे विश्व के स्तर पर पुरुष के समकक्ष स्थान दिलाना। नारीवाद वुल्फ ऑफ फ्राइड के सिद्धान्तों को निरस्त करके लैंगिक समानता का पक्षधर है; शक्ति, योग्यता, कार्यक्षमता अथवा अन्य किसी भी दृष्टि से नारी पुरुष से निम्नतर नहीं है। आज महिलाएं जिस अधीनस्थ और अवपीड़ित स्थिति में हैं उसका कारण प्रकृति नहीं, वरन् समाजीकरण है। अतः पुरुष के समकक्ष स्थिति नारी का हक है अधिकार है। नारी इस स्थिति को प्राप्त कर सके, इसके लिए नारीवाद सभी स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों में वृद्धि की मांग करता है। नारी को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुष के समकक्ष स्थान प्राप्त करने के लिए एक लम्बा और कठिन रास्ता तय करना होगा तथा लक्ष्य की प्राप्ति नारी एकता और नारी सशक्तिकरण के आधार पर ही सम्भव है। अतः नारीवाद इस बात का आह्वान करता है कि पैतृक संरचना के चलते पुरुष प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त कर समाज में समानता और सम्मान का स्थान प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए तथा महिला सशक्तिकरण के लिए परस्पर करना चाहिए। इस प्रकार एक पंक्ति में नारीवाद, नारी समानता (पुरुष से समानता), नारी एकता और नारी – सशक्तिकरण का आन्दोलन है। नारीवाद की मांग है कि नारी को अपना हक (समानता का हक), अपने अधिकार और अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व चाहिए। नारीवाद एक विश्वव्यापी आन्दोलन है, कुछ देशों में यह अपने विकास के उच्च स्तर पर है, कुछ देशों में अपेक्षाकृत कम विकसित स्तर पर । नारीवाद वुल्फ और फ्राइड के सिद्धान्तों को निरस्त करके के सिद्धान्त के आधार पर स्त्री पुरूष दोनों को समान धरातल पर स्थापित कर स्त्री को समाज और समस्त व्यवस्था में उसका उचित स्थान दिलाने के लिए तत्पर आन्दोलन है।
सिमोन दिबोवा की प्रसिद्ध पुस्तक ‘The Second Sex’ (1949) में विस्तार से बतलाया गया है कि स्त्री-पुरूष का भेद समाजीकरण का परिणाम है। समाजीकरण (समाज से जुड़े समस्त वातवरण) से उत्पन्न इस स्थिति को दूर का ‘समान व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों की अधिकार के रूप में मांग’ नारीवाद है। दिबुवा का मुख्य सिद्धान्त है—’ A woman (weak woman) is made, not born. ‘ नारीवाद पुरुष विरोधी आन्दोलन नहीं है, यह तो यथास्थितिवाद विरोधी आन्दोलन है। परिस्थितियों का लाभ उठाकर जिन पुरुषवादी ताकतों ने शक्ति प्राप्त कर ली है, नारीवाद उन पुरुषवादी ताकतों की सत्ता का विरोध करता है, पुरुषवादी ताकतों द्वारा स्त्री के प्रति किए गए और किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करता है। सत्ता का यह विरोध, नारी और पुरुष, दोनों के लिए था और है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुरुषवादी ताकतों में केवल पुरुषों का एक वर्ग ही नहीं, वरन् महिलाओं का एक वर्ग भी सम्मिलित रहा है। पुरुषवादी तत्व महिलाओं की सहायता से महिलाओं पर अत्याचार कर पाए हैं। एक अन्य बात यह है कि पश्चिमी देश हो या भारत नारीवादकी पहले पुरुषों द्वारा ही गई है इस कारण इसे पुरुष विरोधी आन्दोलन नहीं वरन् पैतृक समाज और पुरुषवाद के विरुद्ध आन्दोलन समझा जाना चाहिए।
नारीवाद के लक्षण और लक्ष्य प्राप्ति (विस्तृत व्याख्या)
नारीवाद स्त्री-पुरुष की समानता का आन्दोलन समानता और समाज जीवन के विविध क्षेत्र हैं तथा विविध क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष समानता की विस्तृत इस प्रकार है:
1. नारीवाद और परिवार
नारीवाद मैरिज सिस्टम या विवाह संस्कार (एक स्त्री और एक पुरुष के बीच काम सम्बन्धों को मर्यादित करने की व्यवस्था) और परिवार संस्था का ध नहीं है वरन् इस बात पर बल देता है कि परिवार का मूल आधार पुरुष के प्रति स्त्री का समर्पण नहीं वरन् पुरुष और स्त्री दोनों का एक-दूसरे के प्रति समर्पण और पति-पत्नी के बीच समानता या स्त्री-पुरुष की समानता होनी चाहिए। नारीवाद पुरुष को धिक्कारना नहीं हैं, पुरुष को अस्वीकार करना नहीं हैं पुरुष को केवल समानता, पूर्ण समानता के आधार पर स्वीकार करना है। नारीवाद विवाह विरोधी या परिवार विरोधी तो नहीं है, लेकिन इस बात पर अवश्य ही बल देता है कि विवाह और परिवार नारी के लिए केवल उतनी ही सीमा तक आवश्यक है, जितनी सीमा तक यह पुरूष के लिए आवश्यक है। यदि कोई स्त्री अकेली रहती है, उसने विवाह संस्कार और परिवार संस्था को नहीं अपनाया है, तब यह नारी भी उतनी ही प्रतिष्ठित है जितनी प्रतिष्ठित माता या पत्नी के पद पर असीन कोई नारी हो सकती है। वह विवाह करे या न करे, परिवार संस्था को अपनाये या न अपनाये परिवार के बीच रहे या अकेली रहे अपने जीवन से जुड़ी इन बातों के सम्बन्ध में सोचने और निर्णय लेने का अधिकार केवल उसे है, केवल उसे ही हो सकता है। समाज को वह अधिकार हो ही नहीं सकता कि वह अपनी मान्यताएं और विश्वास नारी पर लादे ।
2. नारीवाद और सामाजिक जीवन या कार्य व्यवहार के विविध क्षेत्र
खेत खलिहान, फैक्ट्री, सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय, व्यापार और रोजगार से जुड़े ये सभी क्षेत्र जीवन के विविध क्षेत्र है। मध्यम तथा उच्च वर्ग में पुरुषवाद और पुरुषवाद से जुड़े सामन्ती संस्कार सामान्यता इस बात पर बल देते रहे हैं कि नारी घर ही चारदीवारी के बीच रहकर पति की सेवा, परिवार के सभी सदस्यों की सेवा देखभाल और बच्चों का पालन-पोषण करे घर के बाहर जीवन के विविध क्षेत्रों में पुरुषों के समान कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं है। नारीवाद इस बात पर बल देता है कि योग्यता और क्षमता की दृष्टि से, नारी किसी भी रूप में पुरुष से कम श्रेष्ठ नहीं है तथा उसे आवश्यक शिक्षा, ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रतियोगी जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान स्तर पर कार्य करने का अधिकार होना चाहिए। वह पुरुष से प्रतियोगिता करने की क्षमता रखती है तथा उसे यह अधिकार प्राप्त है।
अब पुरुषवाद से जुड़ी एक प्रवृत्ति यह जन्म ले रही है कि नारी नौकरी या अन्य कोई कार्य करें, परिवार के लिए अर्थोपार्जन करे लेकिन साथ ही उसे घर-परिवार के सभी कार्यों का बोझ उठाना होगा। वह पति से इस सम्बन्ध में सहयोग की अपेक्षा न रखे। नारीवाद इस प्रवृत्ति का विरोध करता है; पति से पत्नी के प्रति, उसके सभी कार्यों में सहयोग की अपेक्षा करता है, इसे नारी का अधिकार मानता है।
3. नारीवाद और राजनीति
पुरुषवाद सदैव ही इस बात पर बल देता रहा है कि नारी और राजनीति दो बेसल स्थितियां हैं। राजनीति नारी का कार्यक्षेत्र नहीं हो सकता और प्रकृति ने नारी को राजनीति में भागीदारी निभाने की क्षमता प्रदान नहीं की है। नारीवाद इन मान्यताओं का विरोध करता है और इस बात पर बल देता है कि राजनीति में नारी को लगभग बराबरी की भागीदारी (कम-से-कम एक-तिहाई भागीदारी अवश्य ही) प्राप्त होनी चाहिए। महिलाएं न केवल राजनीति में भाग लेने की योग्यता और क्षमता रखती हैं श्रीमती भण्डारनायके, माग्रेट थैचर और गोल्डा मायर, आदि महिलाओं ने जिस सुयोग्य नेतृत्व का परिचय दिया, उससे यह बात प्रमाणित हो जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक व्यावहारिक होती हैं, अधिक मर्यादित आचरण की प्रवृत्ति रखती हैं अतः उनकी अधिक भागीदारी राजनीति के खेल और राजनीतिक व्यवस्था को अधिक मर्यादित करेगी, अनुशासित करेगी तथा समस्त राजनीति और व्यवस्था को उद्देश्यपूर्ण बना देगी। महिलाएं जो विश्व की लगभग 50 प्रतिशत आबादी हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा समस्त जीवन व्यवस्था में भारी सुधार की आवश्यकता है; यह तभी सम्भव जबकि राजनीति में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व और अधिक भागीदारी प्राप्त हो। नारीवाद इस बात पर बल देता है कि न केवल राजनीति वरन् समाज में निर्णय लेने वो शीर्ष पदों पर महिलाएं प्रतिष्ठित हों, उन्हें अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। नारीवाद की मान्यता यह भी है कि राजनीति में न केवल महिलाओं को वरन् ऐसी महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, जिनकी अपनी पहचान हो, जो यह स्थिति अपनी योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर प्राप्त करें। ऐसी महिलाओं के प्रतिनिधित्व से उद्देश्य प्राप्ति हो पाना कठिन है जिन्होंने राजनीति में अपना स्थान किसी प्रभावशाली पुरुष की पत्नी, पुत्री, मित्र या ऐसे ही किसी आधार पर प्राप्त किया है।
4. नारी एकता और नारी-नारी सहयोग
नारीवाद इस बात पर बल देता है कि यदि नारी को उत्थान और विकास की दिशा में आगे बढ़ना है तो यह कार्य नारी एकता और संगठन तथा स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी-नारी सहयोग के आधार पर ही सम्भव है। मूल बात यह है कि किसी एक जाति, धर्म और वर्ग की नारी का नहीं वरन् समस्त नारी जाति का शोषण हुआ है, सभी देशों में कम अधिक रूप में शोषण की यह स्थिति है अतः नारी को अन्य सभी बातें भूलकर अपने नारी होने की बात को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर नारी आन्दोलन को बांटने की कोई भी चेष्टा नारीवाद की मूल अवधारणा के विरुद्ध और नारीवाद के लिए घातक है।
5. नारीवाद और लक्ष्य प्राप्ति हेतु कानून निर्माण एवं प्रशासनिक व्यवस्था
नारीवाद इस बात पर बल देता है कि परम्परागत रूप में जो कानून चले आ रहे हैं, वे पुरुषवादी सोच के परिणाम हैं और उनका निर्माण पुरुष वर्ग की सत्ता को बनाए रखने के लिए किया गया है, अतः इन कानूनों में भारी बदलाव की आवश्यकता है। परम्परागत रूप में बच्चे या व्यक्ति की पहचान उसके पिता से होती है, नारीवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति की पहचान उसकी माता और पिता, दोनों से होनी चाहिए तथा अकेली माता के नाम से भी व्यक्ति की पहचान को पूर्ण वैधता तथा समाज में सम्मान की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। विवाह तलाक, जमीन और सम्पत्ति के उत्तराधिकार के प्रसंग में सभी स्तरों पर महिला को पुरुष के समान अधिकार और समान स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। दहेज हत्या और कन्या विक्रय, दोनों ही स्थितियों का न केवल कानूनन निषेध होना चाहिए, वरन् इन कानूनों को आवश्यक कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा में ‘भ्रूण हत्या निषेध कानून’ आवश्यक कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। ‘स्त्री का किसी भी रूप में यौन शोषण न हो’ इसके लिए कानून और प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। बलात्कारी और यौन अपराधी को दण्डित करने के लिए समस्त कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चालाक और साधन सम्पन्न व्यक्ति के लिए भी सजा से बच पाना सम्भव न रहे; समस्त पुलिस कार्यवाही और न्यायिक सुनवाई ऐसे रूप में होनी चाहिए कि नारी स्वयं को अपमानित न समझे, यौन यातना और बलात्कार के बाद उसे पुलिस कार्यवाही और न्यायिक सुनवाई के नाम पर यातनाओं के दौर से न गुजरना पड़े। राज्य के द्वारा कन्या महिला शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा योग्यतानुसार उनके रोजगार के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जाने चाहिए। अकेली रहने वाली महिलाओं को राज्य और समाज द्वारा पूरी सुरक्षा, पूरी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें पूरा सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए।
इसे भी पढ़े…
- राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की परिभाषा | राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व
- एक राजनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के गुण और दोष
- एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त की सत्यता का विवेचन कीजिए।
- अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए।
- अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।