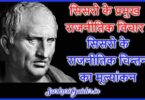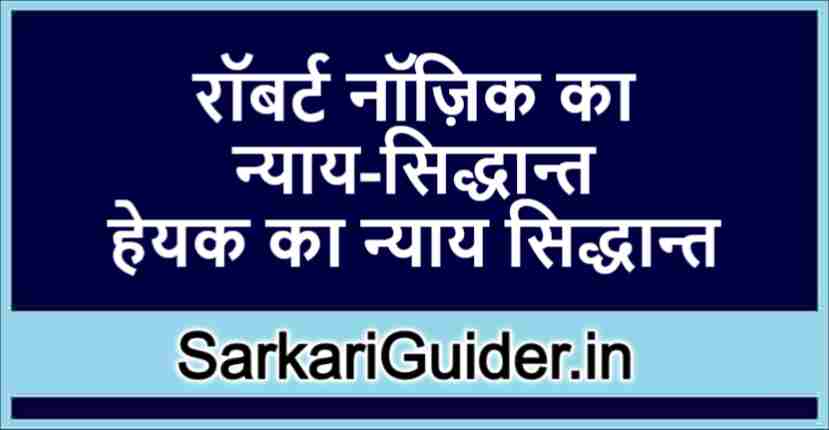
रॉबर्ट नॉज़िक का न्याय-सिद्धान्त
इधर रॉबर्ट नॉज़िक (1938-2002) ने अपनी चर्चित कृति ‘एनार्की, स्टेट एण्ड युटोपिया’ (अराजकता, राज्य और कल्पनालोक) (1974) के अन्तर्गत न्याय के दो तरह के सिद्धान्तों में अन्तर किया है। एक ओर न्याय के ऐतिहासिक सिद्धान्त हैं; दूसरी ओर साध्यमूलक सिद्धान्त हैं। ऐतिहासिक सिद्धान्तों के अनुसार, लोगों की अतीत परिस्थितियों और अतीत कार्यों के आधार पर उनके वर्तमान अधिकार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। इसके विपरीत, साध्यमूलक सिद्धान्तों के अनुसार, लोगों के अधिकार किन्हीं विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के लिए, उपयोगितावाद एक साध्यमूलक सिद्धान्त है जो ‘अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख’ के लक्ष्य को सबके अधिकारों का उपयुक्त आधार मानता है। नॉज़िक ने इस सिद्धान्त की तीव्र आलोचना की है।
स्वयं नॉज़िक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धान्त को अपने तर्क का आरम्भिक ‘बिन्दु स्वीकार किया है। इसके अनुसार, यदि वैयक्तिक सम्पत्ति की वर्तमान व्यवस्था अतीत के उचित अभिग्रहण या हस्तान्तरण का परिणाम है, अर्थात् इसमें छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसे न्यायपूर्ण मान लेना चाहिए। परन्तु यदि अतीत में सम्पत्ति के अनुचित अभिग्रहण के कारण कोई अन्याय हुआ है तो उसका परिष्कार उचित होगा। इस प्रक्रिया को नॉज़िक ने परिष्कार का सिद्धान्त कहा है। परन्तु उसका विचार है कि परिष्कार के सिद्धान्त को बहुत दूर तक लागू नहीं किया जा सकता। यदि हम पुरानी सारी त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे तो अनेक विवाद पैदा हो जाएंगे। इन्हें सुलझाने का प्रयत्न करने पर ये विवाद बढ़े ही चले जाएंगे। अतः हमें यह मान लेना चाहिए कि भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को अपनी वर्तमान सम्पत्ति अपने पास रखने का अधिकार है, और समाज में सम्पदा के फैलाव को किसी नए रूप में ढालने का कोई औचित्य नहीं हैं।
नॉज़िक के अपने सिद्धान्त को न्याय का अधिकारिता सिद्धान्त कहा जाता है। इसमें यह मानकर चलते हैं कि प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत जो व्यक्ति जिस-जिस वस्तु का अधिकारी है, उसे उसकी सहमति के बिना किमी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। फिर, विभिन्न मनुष्य अपनी-अपनी प्रतिभा और प्रयास से सामाजिक उत्पादन में भिन्न-भिन्न योगदान करते हैं, इसलिए उन्हें भिन्न-भिन्न पुरस्कार प्राप्त होना स्वाभविक है। नॉज़िक ने तर्क दिया है कि समाज में उत्पादन के स्तर पर जो असमानताएं पाई जाती हैं, उन्हें वितरण के स्तर पर बदलने का प्रयत्न विनाशकारी होगा। संसार में कोई भी वस्तु शून्य से पैदा नहीं होती, बल्कि समाज की सम्पदा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के परिश्रम का परिणाम है। लोग व्यापार के द्वारा अपनी सम्पत्ति बढ़ाते हैं या उसे खो देते हैं। सम्पत्ति का वर्तमान वितरण उनके स्वैच्छिक विनिमय का परिणाम है। न्यूनतम राज्य उनके इस अधिकार की रक्षा करता है। इस प्रक्रिया में किसी तरह के हस्तक्षेप काअर्थ होगा, व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन। अतः राज्य के समस्त कल्याणकारी कार्यक्रम सर्वथा अवैध हैं।
संक्षेप में, नॉज़िक का अधिकारिता सिद्धान्त मोटे तौर पर तीन सिद्धान्त-तत्त्वों को मान्यता देता है-
(1) न्यायपूर्ण हस्तान्तरण का सिद्धान्त- इसका अर्थ यह है कि न्यायपूर्ण तरीके से जिस वस्तु का अभिग्रहण किया गया हो, उसे स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरित किया जा सकता है;
(2) मूलतः न्यायपूर्ण अभिग्रहण का सिद्धान्त – इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति जिस वस्तु का स्वामी है, उसे उसने न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया हो, तभी उसे वह स्वेच्छापूर्णक हस्तान्तरित करने का अधिकारी माना जाएगा; और
(3) अन्याय के परिष्कार का सिद्धान्त- इसका अर्थ यह है कि यदि कहीं अन्यायपूर्ण तरीक़े से किसी वस्तु का अभिग्रहण या हस्तान्तरण किया गया हो तो ऐसी स्थिति का उचित प्रतिकार करना चाहिए।
इस सारी तर्क-श्रृंखला से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि लोगों की वर्तमान सम्पत्ति न्यायपूर्ण तरीक़े से प्राप्त की गई हो तो उसके न्यायपूर्ण वितरण के लिए यह सूत्र अपनाना चाहिए
‘हरेक से उतना जितना वह देना चाहे, हरेक को उतना जितना उसे कोई देना चाहे ।
‘यह सूत्र बाज़ार में होने वाले लेन-देन के तौर-तरीके को ही व्यक्त करता है। इसे राजनीतिक के क्षेत्र में उतार कर नॉज़िक ने ‘न्यूनतम राज्य’ का समर्थन किया है। ऐसे राज्य का कार्यक्षेत्र अत्यन्त सीमित और संकुचित होगा। वह लोगों को छल-बल और चोरी से संरक्षण प्रदान करेगा; अनुबन्धों को लागू करेगा; इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। यदि वह इससे बाहर कुछ करेगा तो यह व्यक्तियों को विवश करने के तुल्य होगा जो कि उनके अधिकारों का हनन होगा। अतः राज्य को न तो सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए; न सार्वजनिक स्वास्थ्य या परिवहन की; न सड़कें बनवानी चाहिए। यदि वह ऐसा कुछ करेगा तो इसके लिए लोगों की इच्छा के विरुद्ध उन पर कर लगाना पड़ेगा जिससे न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा। नॉज़िक यहां तक मानता है कि यदि निर्धन एवं विकलांग भूखे मर रहे हों तो उन्हें बचाने के लिए धनवान एवं समर्थ लोगों पर कर लगाना अन्यायपूर्ण होगा।
नॉज़िक का विचार है कि यदि व्यक्तियों के अधिकारों को किसी नए लक्ष्य के अनुरूप ढालने की कोशिश की जाएगी तो वह स्वतन्त्रता के लिए विनाशकारी होगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई सरकार ‘सबके लिए समान आय’ का नियम लागू करना चाहे तो उससे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता का लगातार हनन होने लगेगा। फिर, व्यक्तियों के स्वैच्छिक विनिमय के फलस्वरूप सम्पत्ति की जो नई व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, उसे सरकार के पूर्वनिर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ढालने का प्रयत्न सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा देगा।
नॉज़िक के अनुसार, सम्पत्ति के ‘उचित अभिग्रहण’ और ‘स्वैच्छिक विनिमय’ पर प्रतिबन्ध लगाने का एक ही आधार युक्तियुक्त होगा। वह यह कि लोगों की इन गतिविधियों के कारण दूसरों की स्थिति पहले से ख़राब न हो जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु के सम्पूर्ण स्रोत को अपने अधिकार में लेना चाहे जो मानव-जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक है तो उस पर प्रतिबन्ध लगाना उपयुक्त होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत हो तो किसी व्यक्ति को उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती। परन्तु यदि कोई लोकप्रिय खिलाड़ी या कलाकार अपने कार्य-प्रदर्शन की मनमानी क़ीमत मांगता है, और लोग उसे देने को तैयार हों तो उसे जितनी भी विशाल धनराशि प्राप्त हो, उस पर उसका पूर्ण अधिकार होगा क्योंकि इसमें छल या बल का प्रयोग नहीं हुआ है; उसने वही लिया जितना लोग स्वेच्छा से देते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी प्राणाघातक रोग का उपचार ढूंढ़ ले तो उसे इसकी मनचाही क्रीमत मांगने का पूरा हक़ है क्योंकि वह इस आविष्कार के लिए किसी का ऋणी नहीं है, और अपने आविष्कार की क़ीमत मांग कर वह दूसरों के पहले से ख़राब स्थिति में नहीं डाल रहा है। उसकी स्थिति की तुलना ऐसी इजारेदारी से नहीं की जा सकती जो दूसरों को उनके जीवन के आधार से वंचित कर रही हो। परन्तु यदि काई व्यक्ति दूसरों को प्राणघातक रोग का उपचार ढूंढ़ने से सचमुच रोकता है तो यह अन्याय होगा ।
इस तरह नॉज़िक ने अपनी अनोखी तर्क-शैली के आधार पर शुद्ध प्रतिस्पर्धात्मक समाज को न्यायपूर्ण समाज के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें विवश और वंचित वर्गों को कोई सहायता प्राप्त होने की गुंजाइश नहीं है। यह बात ध्यान देने की है कि जहां राल्स का न्याय-सिद्धान्त सबसे निर्धन और सबसे ज़रूरतमन्द व्यक्ति को सबसे पहले सहायता पहुँचाने की मांग करता है, वहां नॉज़िक का न्याय-सिद्धान्त ऐसे व्यक्ति मर-खप जाने के लिए छोड़ देता है।
हेयक का न्याय सिद्धान्त
रॉबर्ट नॉज़िक की तरह एफ. ए. हेयक (1899-1992) भी प्रक्रियात्मक न्याय का प्रबल समर्थक है। हेयक ने तात्त्विक न्याय के विचार का खण्डन करते हुए अपनी चर्चित कृति ‘लॉ, लेजिस्लेशन एण्ड लिबर्टी : द मिराज ऑफ़ सोशल जस्टिस’ (क़ानून, विधि-निर्माण और स्वतन्त्रता : सामाजिक न्याय की मृगतृष्णा) (खण्ड दो) (1976) के अन्तर्गत यह तर्क दिया है कि ‘सामाजिक न्याय’ का विचार ही निरर्थक है। न्याय वस्तुतः मनुष्य के आचरण की विशेषता है; कोई समाज न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण नहीं हो सकता। यदि समानता के हित में स्वतन्त्रता में कटौती की जाती है तो जीवन-सामग्री के अन्यायपूर्ण वितरण के प्रश्न पर तनाव, कलह और विवाद अवश्य पैदा होंगे। न्याय की तलाश केवल प्रक्रिया का विषय है जिसका ध्येय स्वतन्त्रता को बढ़ावा देना है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने-अपने ज्ञान और अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार अपने-अपने हितसाधन का अधिकतम अवसर मिलना चाहिए।
देखा जाए तो स्वयं हेयक ने न्याय का कोई विशेष सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया है। उसने केवल स्वतन्त्रता का वर्चस्व स्थापित करने के ध्येय से सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर विशेष रूप से प्रहार किया है। उसने तर्क दिया है कि समाज के पास इतने सीमित संसाधन हैं कि उनसे सबकी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती। सामाजिक न्याय की नीति अपनाने पर अधिकारीतन्त्र को इन संसाधनों के मनमाने वितरण की शक्ति प्राप्त हो जाएगी जिससे व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को क्षति पहुँचेगी। इसके अलावा, समाज में भिन्न-भिन्न हित समूह अपने-अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन सीमित संसाधनों में से अपने-अपने हिस्से की मांग करने लगेंगे। जो हित समूह जितना शक्तिशाली होगा, वह उतना बड़ा हिस्सा ले जाएगा। इस तरह सामाजिक न्याय की आड़ में अयोग्य लोगों को समाज की सम्पदा में से अनुचित हिस्सा बटोरने का मौक़ा मिल जाएगा। इससे योग्य लोगों को नुक़सान होगा। वे हतोत्साह होकर परिश्रम से विमुख हो जाएंगे, और सामाजिक प्रगति को धक्का लगेगा।
इसे भी पढ़े…
- राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की परिभाषा | राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व
- एक राजनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के गुण और दोष
- एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त की सत्यता का विवेचन कीजिए।
- अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए।
- अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।