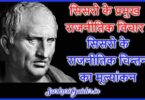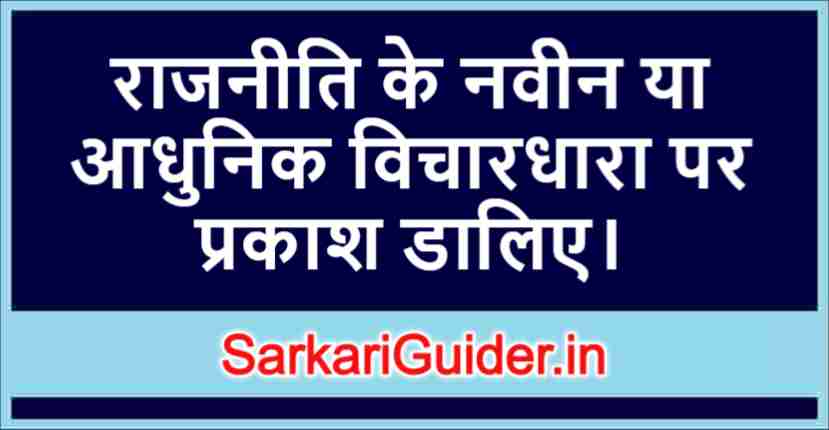
राजनीति के नवीन या आधुनिक विचारधारा
राजनीति की चिरसम्मत धारणा के विपरीत, आज के युग में राजनीति का प्रयोग क्षेत्र तो सीमित हो गया है, परन्तु इसमें भाग लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में, आज राजनीति के अध्ययन में मनुष्य के सामाजिक जीवन की समस्त गतिविधयों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि केवल उन गतिविधियों पर विचार किया जाता है तो सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं। परंतु आज के युग में सार्वजनिक नीतियां और निर्णय इने-गिने शासकों, विधायकों या सत्ताधारियों की इच्छा को व्यक्त नहीं करते बल्कि समाज के भिन्न भिन्न समूहों की परस्पर क्रिया के फलस्वरूप उभरकर सामने आते हैं। इस तरह राजनीति जनसाधारण की उन गतिविधियों का संकेत देती है जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न समूह अपने-अपने परस्पर विरोधी हितों में तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। यह जरूरी नहीं कि इससे सचमुच न्यायसंगत समाधान ही निकले। कुछ समूह अधिक संगठित, अधिक साधन-संपत्र, अधिक मुखर और अधिक व्यवहार कुशल होते हैं। अतः वे अपने हितों को अन्य समूहों के हितों से ऊपर रखने में सफल हो जाते हैं जिससे सामाजिक जीवन में असंतुलन पैदा हो जाता है। परंतु यह आशा की जाती है कि राजनीति की प्रक्रिया में अन्य समूहों को अपने हितों को संगठित करने और बढ़ावा देने का अवसर मिलता रहेगा जिससे आगे चलकर न्यायसंगत समाधान की संभावना बनी रहेगी।
परंपरागत राजनीतिशास्त्र का मुख्य सरोकार ‘राज्य’ से था, इसलिए इसकी परिभाषा ‘राज्य ‘के विज्ञान’ के रूप में दी जाती थी। राजनीतिशास्त्र के परंपरागत विद्वानों और लेखकों ने अपना ध्यान मुख्य रूप इन समस्याओं पर केंद्रित कियाः (क) राज्य के लक्षण, मूलतत्त्व और संस्थाएँ क्या हैं: और (ख) ‘सर्वगुण संपन्न राज्य का स्वरूप कैसा होगा ? परंतु आधुनिक लेखक यह अनुभव करते हैं कि ‘राजनीति’ मानव जीवन की एक विशेष गतिविधि है; यह केवल ‘राज्य’ की कामना करते हैं, इसलिए ये सब मूल्यों के उदाहरण हैं। दूसरे शब्दों में, मूल्य ऐसी इष्ट वस्तुएँ, लाभ या सेवाएँ हैं जिन्हें हर कोई पाना चाहता है, परंतु उनकी इतनी कमी है कि उन्हें कोई-कोई ही पा सकता है। अतः इनके मामले में समाज के अंदर ‘एक अनार सौ बीमार’ वाली कहावत चरितार्थ होती है।
आबंटन से उसका अभिप्राय है, विभिन्न व्यक्तियों या समूहों में इन वस्तुओं का वितरण या बँटवारा, अर्थात् यह निर्णय करना कि किसे क्या मिलेगा? यह कार्य नीति के द्वारा संपन्न किया जाता है जिसमें ‘निर्णयों का समुच्चय’ आ जाता है। दूसरे शब्दों में, जैसे बहुत सारे निर्णयों को मिलाकर नीति तैयार की जाती है, और समाज में मूल्यवान वस्तुओं, लाभों या सेवाओं का बँटवारा इस नीति के अनुसार किया जाता है। निर्णय का अर्थ है, अनेक विकल्पों में से एक का चयन । उदाहरण के लिए, जब बसें थोड़ी हों और बहुत सारी बस्तियों के लोग बस सेवा की मांग कर रहे हों, तब बसें कहाँ-कहाँ। से चलाई जाएं- इस बारे में अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हो सकते हैं। इनमें से उपयुक्त प्रस्ताव के चुनाव कार्यान्वित करना भी शामिल है। ‘को ‘निर्णय’ कहेंगे। ‘नीति’ में ‘निर्णय’ तक पहुँचना और उसे
अब ‘आधिकारिक’ शब्द की परिभाषा देना रह जाता है। ईस्टन के शब्दों में, आधिकारिक का अर्थ यह है कि कोई नीति जिन लोगों के लिए बनाई जाती है, लागू की जाती है या वह जिन्हें । प्रभावित करती है, वही लोग उसका पालन करना आवश्यक या उचित समझते हों। दूसरे शब्दों में, आधिकारिक सत्ता का ध्यये लोगों को बाध्य करना या विवश करना नहीं है। इसका अर्थ है, किसी विशेष निर्णय या कार्रवाई को लागू करने क लिए लोगों से सहर्ष आज्ञापालन कराने की क्षमता।
जब हम राजनीति की परिभाषा ‘मूल्यों’ के अधिकारिक आबंटन के रूप में देते हैं, तब हम उसे एक सार्वजनीन सामाजिक घटना के रूप में पहचानते हैं। दूसरे शब्दों में, राजनीति एक विश्वव्यापी गतिविधि है। किसी भी समाज में अभीष्ट वस्तुएं, लाभ और सेवाएं, इत्यादि थोड़ी होती हैं और उनकी मांग करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। अतः वहां ऐसी आधिकारिक सत्ता की जरूरत होती है जो परस्पर विरोधी मांगों को सामने रखकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिसे सब लोग स्वीकार कर ले। इसका अर्थ यह नहीं कि सबकी मांगे कर दी जाती हैं, या कोई सामाधान हमेशा के लिए स्वीकार कर लिया जाता है। वास्तव में, एक समाधान स्वीकार कर लेने के बाद नई मांगें नए-नए रूपों में प्रस्तुत की जाती हैं, और फिर नए समाधान की तलाश शुरू हो जाती है। अतः राजनीति एक निरंतर प्रक्रिया है। हम ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें राजनीति शुरू न हुई हो, या समाप्त हो गई हो। राजनीति के इस दृष्टिकोण को हम साधारणतः उदारवादी दृष्टिकोण के रूप में पहचानते हैं। राजनीति का यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है।
निष्कर्ष राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत यह मानकर चलते थे कि सामाजिक जीवन का लक्ष्य या ध्येय पहले से नियत या निर्धारित है, और समाज के सदस्यों को पहले से निश्चित व्यवस्था के भीतर अपने-अपने कर्तव्यां का पालन करना चाहिए। किसी को उससे मतभेद प्रकट करने या कोई नया रास्ता सुझाने का अधिकार नहीं था। राजनीति का आधुनिक दृष्टिकोण प्राचीन दृष्टिकोण से इसलिए भिन्न है कि इसमें मतभेद, संघर्ष या द्वंद्व को सामाजिक जीवन का स्वाभाविक लक्ष्ण माना जाता है। इस मतभेद को दबाने पर बल नहीं दिया जाता बल्कि इसका समाधान ढूंढने पर बल दिया जाता है।
राजनीति के आधुनिक दृष्टिकोण में ये विचार निहित हैं:
(क) समाज में मूल्यवान वस्तुओं, सेवाओं, लाभों और अवसरों में से अपना-अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूहों में मतभेद, खींचातानी और प्रतिस्पर्धा पाई जाती है:
(ख) परंतु इन वस्तुओं का बँटवारा कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या हो इस बारे में सहमति पाई जाती है, अर्थात् समाज के सदस्य ऐसे नियम और कार्यविधि स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनके अनुसार उनके परस्पर विरोधी दावों को सुलझाया जा सके;
(ग) एक बार जो बँटवारा कर दिया जाता है, लोग उसे स्वीकार करके उसका सम्मान करते हैं; नियम तोड़ने वाले को दंड दिया जाता है, उसका उपहास किया जाता है, या उसकी अंतरामा उसे कचोटती है;
(घ) परंतु इस बँटवारे से सब लोग संतुष्ट नहीं हो जाते; नई मांगे प्रस्तुत करने, नए समाधान ढूंढ़ने और नई व्यवस्था स्थापित करने के साधन और अवसर हमेशा विद्यमान रहते हैं।
ज्यॉफ्री के. रॉबर्ट्स ने ‘ए डिक्शनरी ऑफ़ पॉलिटिकल एनालिसिस’ (राजनीति- विश्लेषण शब्दकोश) के अंतर्गत राजनीति की आधुनिक धारणा को इस परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है, जो कि सर्वथा उपयुक्त है: राजनीति एक गतिविधि का संकेत भी देती है, और उस गतिविधि के अध्ययन का संकेत भी देती है। एक गतिविधि के रूप में राजनीति सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत एक प्रक्रिया है। यह जरूरी नहीं कि वह राष्ट्र-राज्य तक ही सीमित हो। इस प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक प्रणाली के लक्ष्य चुने जाते हैं, उन्हें समय की दृष्टि से तथा साधनों के आबंटन की दृष्टि से प्राथमिकता के क्रम में रखा जाता है, और कार्यान्वित किया जाता है। अतः इसमें सहयोग के अलावा संघर्ष के समाधान की आवश्यकता भी होती है। इसके लिए राजनीतिक सत्ता का प्रयोग किया जाता है, और यदि जरूरी हो तो बल-प्रयोग का सहारा भी लिया जाता है। यह अन्य सामाजिक प्रक्रियाओं से इसलिए भिन्न है कि इसका सरोकार समाज के ‘सार्वजनिक लक्ष्यों’ से है जबकि अर्थशास्त्र का सरोकार साधनों के सार्वजनिक या निजी आवंटन से हो सकता है।
इसे भी पढ़े…
- राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रवाद की परिभाषा | राष्ट्रीयता के मुख्य तत्व
- एक राजनीतिक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के गुण और दोष
- एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धान्त की सत्यता का विवेचन कीजिए।
- अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए।
- अधिकारों के वैधानिक सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
- सिद्धान्त निर्माण में डेविड ईस्टन के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर आर्नाल्ड ब्रेख्त के विचार
- सिद्धान्त निर्माण पर कार्ल डायश के विचार
- सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया
- भारत के संविधान की प्रस्तावना एवं प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताएँ
- भारतीय संविधान की विशेषताएँ
- नागरिकता से क्या आशय है? भारत की नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख शर्तें
- राज्यपाल की शक्तियां और कार्य क्या है?
- राज्य शासन में राज्यपाल की स्थिति का वर्णन कीजिए।
- राज्य शासन क्या है? राज्य शासन में राज्यपाल की नियुक्ति एवं पद का उल्लेख कीजिए।
- राज्यपाल की शक्तियां | राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य
- धर्म और राजनीति में पारस्परिक क्रियाओं का उल्लेख कीजिए।