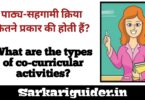वैदिक कालीन या गुरुकुल शिक्षा
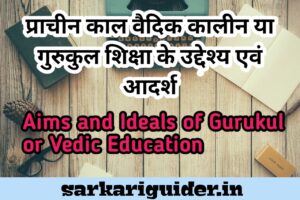
Ancient (Vedic Period) or Gurukul Education
प्राचीनकाल (वैदिक कालीन) या गुरुकुल शिक्षा
Ancient (Vedic Period) or Gurukul Education
प्राचीनकाल (वैदिक कालीन) या गुरुकुल शिक्षा Ancient (Vedic Period) or Gurukul Education – भारतीय सभ्यता एवं शिक्षा की पृष्ठभूमि में वेद ही हैं। वेदों द्वारा हमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता, जीवन और दर्शन का ज्ञान होता है। वेद हमारी वह थाती हैं, जो मानव जीवन के लक्ष्य को अपने में सँजोये हुए हैं। वैदिक काल का विस्तार ईसा पूर्व 2500 से लेकर 500 ई. पूर्व तक माना जाता है। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। अतः वैदिक कालीन शिक्षा को ‘ब्राझण शिक्षा’ एवं ‘हिन्दू शिक्षा’ की संज्ञा भी दी जाती है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। यथा-‘विद्या’, ‘ज्ञान’, ‘बोध’ तथा ‘विनय’। आधुनिक शिक्षाशास्त्रियों के समान प्राचीनकाल में भारतवासियों ने भी ‘शिक्षा’ शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया है।
डॉ. ए. एस. अल्टेकर के अनुसार – ” व्यापक अर्थ में, शिक्षा का तात्पर्य है- व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में, शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है, जो व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती थी। “ भारतीय शिक्षा का आरम्भ प्रकृति की गोद में मानव की मूलभूत जिज्ञासा की शान्ति के लिये हुआ था। भारत में शिक्षा के तत्त्व, प्रणाली तथा संगठन का प्रारूप प्राय: वैदिक युग से माना जाता है।
डॉ. अल्टेकर के अनुसार – “ वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का अभिप्राय प्रकाश के स्रोत से रहा है और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित एवं प्रकाशित करता रहा है। “ भारत की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परम्परा विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। आज का भारत जो कुछ है, वह अपनी गत 5000 वर्ष की सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत की देन है। प्राचीन भारत की शिक्षा एवं समाज की जानकारी देने वाले ग्रन्थों में वेदों का पहला स्थान है।
डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी ने कहा है – “ प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्णरूपेण धर्म से प्रभावित देखते हैं। “ प्राचीनकाल में शिक्षा का आधार धर्म तथा धार्मिक क्रियाएँ थीं। वैदिक क्रियाएँ ही शिक्षा का प्रमुख आधार थीं। मानव जीवन धर्म से अनुप्राणित होता था।
गुरुकुल या वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श
Aims and Ideals of Gurukul or Vedic Education
वेदों के युग में शिक्षा का स्वरूप आदर्शवादी था। ईश्वर भक्ति, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व के विकास, संस्कृति, राष्ट्र तथा समाज के विकास के प्रति अभिवृत्ति विकसित करने पर आचार्यजन बल देते थे। डॉ. अल्टेकर ने इसी सन्दर्भ में कहा है-“ईश्वर भक्ति, धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की अभिवृद्धि, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे।” वैदिक युग में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श मानव को उसके आत्मिक विकास की ओर ले जाते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य में ऐसी क्षमता और योग्यता का सृजन करना था, जिसके माध्यम से वह सत्य का ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त कर सके। अत: गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य तथा आदर्श निम्नलिखित थे-
1. व्यक्तित्व का समन्वित विकास –
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के अनुसार मानव का मुख्य उद्देश्य आत्म-ज्ञान अथवा ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिये। इसके लिये धार्मिक भावना का विकास किया जाना आवश्यक है। अत: प्रारम्भिक शिक्षा में विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था, नियमित सन्ध्या एवं धार्मिक उत्सव आदि को विशेष महत्त्व दिया जाता था। छात्र के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था, जिससे उसके व्यक्तित्व का समन्वित विकास हो सके। इन तीनों दृष्टिकोण में आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर अधिक बल दिया जाता था। मानसिक विकास के लिये प्रश्नोत्तर, वाद-विवाद तथा शास्त्रार्थ का प्रावधान था, जिससे विद्यार्थियों में चिन्तन, मनन तथा व्यक्तित्व का विकास आदि मानसिक शक्तियों को विकसित किया जा सके।
2. स्वस्थ चरित्र का निर्माण –
वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप चरित्र का निर्माण करना था। अतः सरल जीवन, सदाचार, सत्याचरण एवं अहिंसात्मक व्यवहार और ब्रह्मचर्य उनके दैनिक जीवन के अंग थे। इसके लिये वर्णाश्रम धर्म का पालन करना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिये आवश्यक था।
3. सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण –
वैदिक काल में विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परम्पराओं का संरक्षण करें तथा उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित कर सकें। यह कार्य शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। वैदिक काल में व्यक्ति के व्यवसाय एवं कार्यों का आधार वर्ग व्यवस्था थी। पिता जो व्यवसाय करता था, उसकी शिक्षा पुत्र को देता था। पुत्र भी पारिवारिक संस्कृति तथा परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने में विश्वास करते थे।
4. व्यावसायिक कुशलता का विकास –
वैदिक कालीन जीवन संघर्षमय था। इस संघर्षमय स्थिति में यह आवश्यक था कि शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो जिससे व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप व्यवसाय का चयन कर सके तथा व्यावसायिक कुशलता में वृद्धि कर स्वयं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना सके। इसलिये विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों तथा जीविकोपार्जन से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान की जाती थी। अत: शिक्षा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही नहीं रहा वरन् भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना भी हो गया था।
5. दायित्वों के निर्वाह की क्षमता –
गुरुकुल शिक्षा व्यक्ति को उसके स्वयं के प्रति कर्त्तव्यों का बोध तो कराती ही थी, साथ ही साथ सामाजिक दायित्वों का भी बोध कराती थी। यथा- परोपकार, अतिथि सत्कार, दीन-दुःखियों की सेवा, गुरु तथा वृद्धजनों का सम्मान एवं सेवा आदि प्रकार के कार्य। अत: शिक्षा का दायित्व था कि वह व्यक्ति में नागरिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने की क्षमता का विकास करे।
6. ज्ञान एवं अनुभव पर बल –
गुरुकुलों में विद्यार्थियों को ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने पर बल दिया जाता था। उस समय उपाधि वितरण जैसी प्रथा न थी। छात्र अर्जित योग्यता का प्रश्न विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ द्वारा किया करते थे। गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य अथवा आदर्श केवल पढ़ना नहीं था वरन् मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात् करना भी था। डॉ. आर. के. मुकर्जी के शब्दों में, “वैदिक युग में शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात् करना था।”
7. चित्तवृत्तियों का निरोध –
चित्तवृत्तियों का मार्गान्तीकरण करना, मन को भौतिक ज्ञान से हटाकर आध्यात्मिक जगत् में लगाना तथा आसुरो वृत्तियों पर नियन्त्रण करना वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता था क्योंकि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अनश्वर है, अमर है। अत: आत्मिक उत्थान के लिये जप, तप एवं योग पर विशेष बल दिया जाता था। यह कार्य चित्तवृत्तियों का निरोध करके अर्थात् मन पर नियन्त्रण करके ही सम्भव थे। इसलिये छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। डॉ. आर. के. मुकर्जी के शब्दों में-“वैदिक शिक्षा का उद्देश्य चित्तवृत्ति का निरोध अर्थात् मन में उन कार्यों का निषेध था, जिनके कारण वह भौतिक संसार में उलझ जाता है।”
8. ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता – प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर-भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था, जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति को सम्भव बनाये-“सा विद्या या विमुक्तये” (व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकता थी, जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो) छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना तथा धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था।
Important Links
- शिक्षा का महत्त्व | Importance of Education in Hindi D.el.ed 2nd semester
- शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ | Modern Meaning of Education
- शिक्षा की संकल्पना तथा शिक्षा का प्राचीन अर्थ | Concept & Ancient Meaning of Education
- डॉ. मेरिया मॉण्टेसरी (1870-1952) in Hindi d.el.ed 2nd semester
- फ्रेडरिक फ्रॉबेल (1782-1852) in Hindi d.el.ed 2nd semester
- जॉन डीवी (1859-1952) in Hindi d.el.ed 2nd semester
- रूसो (Rousseau 1712-1778) in Hindi d.el.ed 2nd semester
- प्लेटो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, तथा क्षेत्र में योगदान
- पाठ्यचर्या ( Curriculum) क्या है? पाठ्यचर्या का अर्थ, परिभाषा Curriculum in Hindi