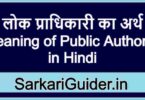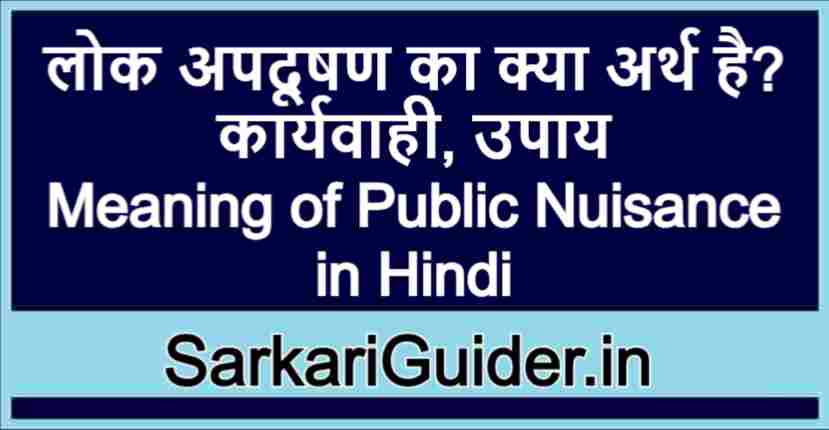
लोक अपदूषण का अर्थ ( Meaning of Public Nuisance in Hindi)
‘लोक अपदूषण’ (public nuisance) की परिभाषा संहिता की धाराओं के अधीन नहीं किया गया है। इसकी परिभाषा साधारण खण्ड अधिनियम (General Clauses Act 1897) की धारा 3 की उपधारा 48 ) में इस प्रकार किया गया है कि लोक-अपदूषण की वही परिभाषा होगी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में है।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268
लोक अपदूषण को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार “लोक-अपदूषण ऐसा कार्य या अवैध कार्यलोप है, जिससे जनता को या उन लोगों को जो आस-पास रहते हैं या सम्पत्ति के अधिभोगी (occupier) है, सामान्य क्षति, खतरा एवं शोध होता है या जिससे उन व्यक्तियों को जिनको किसी सार्वजनिक अधिकार के उपयोग का अवसर प्राप्त होता है, क्षति पहुँचती है, या बाधा, खतरा एवं क्षोभ उत्पन्न होता है।”
धारा 91 के अधीन न केवल लोक-अपदूषण के लिये वाद संस्थित किया जा सकता है अपितु लोक-अपदूषण से भिन्न दोषपूर्ण कार्य (wrongful act) के लिये भी वाद संस्थित किया जा सकता है। संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से ऐसा सम्भव हुआ है।
‘जहाँ एक कम्पनी के सिगरेट के व्यापार-चिन्ह का प्रयोग दूसरी कम्पनी करती है और उससे सिगरेट का विक्रय बढ़ जाता है, वहाँ सिक्किम उच्च न्यायालय ने आई० टी० सी० बनाम श्रीकृष्ण मोक्तान नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि इससे लोक अपदूषण के अन्तर्गत वाद लाने हेतु वाद हेतु नहीं उत्पन्न होता।
जहाँ आवासीय के साथ वाणिज्यिक क्षेत्र में तेल मिल (oil expeller) लगाया गया है, तेल मिल के क्रियाकलाप को रोकने के लिये वाद इस आधार पर संस्थित किया गया है कि यह अपदूषण का निर्माण करेगा |
वहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनील कुमार वर्मा बनाम रघुवीर सिंह नामक वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि मिल के क्रिया-कलाप को मात्र इस अभिकथन पर कि यह अपदूषण फैलायेगा, अन्तरिम आदेश के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। इसके लिये पूर्ण साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी।
विशेष क्षति या हानि
इस धारा के अधीन उन व्यक्तियों के द्वारा भी वाद संस्थित किया जा सकता है जिन्हें लोक-अपदूषण या दोषपूर्ण कार्य से विशेष क्षति भले ही न पहुँची हो । विशेष क्षति से तात्पर्य उस क्षति से है जो किसी व्यक्ति को उससे अधिक पहुँचेगी, जो उस अपदूषण से प्रभावित दूसरे व्यक्ति द्वारा सामान्य रूप से सहन की जाती है।
लोक-अपदूषण के लिये उपाय
लोक-अपदूषण के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध निम्न के प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है |
(अ) आपराधिक विधि के अधीन
(1) दोषी व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है |
(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से 143 द्वारा मजिस्ट्रेट को समरी या संक्षिप्त अधिकार उस लोक-अपदूषण को हटाने के लिये प्राप्त है।
(ब) दीवानी विधि के अधीन
(1) बिना विशेष क्षति दर्शाये संहिता की धारा 91 के अधीन वाद संस्थित किया जा सकता है।
(2) प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा भी जिसे लोक-अपदूषण से विशेष क्षति पहुँची है, वाद संस्थित किया जा सकता है। वाद का संस्थित किया जाना धारा के अधीन (1976) संशोधन के पश्चात्) निम्न द्वारा वाद सस्थित किया जा सकता है |
(अ) राज्य के महाधिवक्ता द्वारा या
(ब) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली है।
1976 से पहले की स्थिति इस धारा के अधीन 1976 के संशोधन से पहले निम्नलिखित वाद संस्थित कर सकते थे (अ) राज्य के महाधिवक्ता, या (ब) दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने महाधिवक्ता की लिखित अनुमति प्राप्त कर लिया था।
इस धारा के अधीन घोषणा
वाद (declaration suit) या व्यादेश-वाद (injunction suit) या किसी अन्य अनुतोष के लिये वाद संस्थित किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत वाद संस्थित करने के लिये अनुमति देने से पहले सावधानी के एक नियम के रूप में न्यायालय को चाहिये कि वह प्रतिवादियों को सूचना दे, परन्तु वह ऐसा करने के लिये बाध्य नहीं है। ध्यान रहे संहिता की धारा 91 (1) में उपलब्ध उपाय लोक उपताप या अन्य दोषपूर्ण कार्य के बारे में है और जो सर्वजन को प्रभावित करती है या प्रभावित कर सकती है, विस्तृत नहीं है। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 307 (5) में उपलब्ध उपाय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 से स्वतन्त्र है और निगम या किसी अन्य व्यक्ति को भी उपलब्ध है।
इसे भी पढ़ें…
- साइबर अपराध क्या है?
- साइबर कैफे किसे कहते हैं?
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर टिप्पणी
- वित्तीय अपराध पर संक्षिप्त लेख
- बाल अश्लीलता क्या है?
- साइबर अश्लीलता क्या है
- हैकिंग कैसे करते हैं?
- हैकिंग क्या है?
- अन्तर्राष्ट्रीय साइबर अपराध की विधि
- साइबर अपराध क्या है?