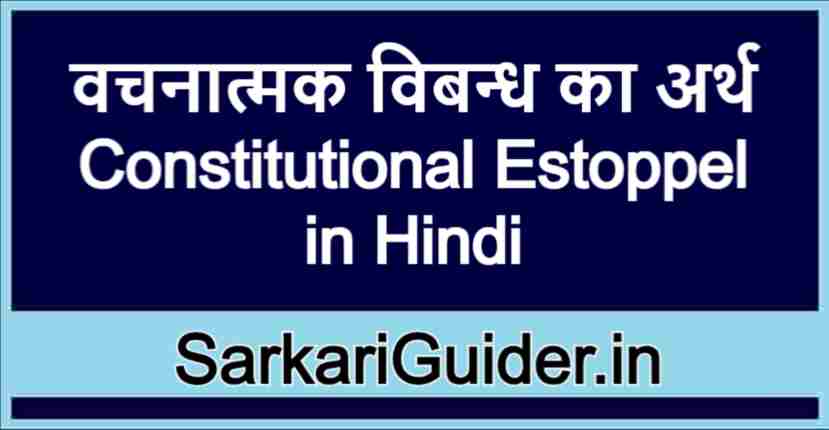
वचनात्मक विवन्ध का अर्थ (constitutional estoppel)
वचनात्मक विबन्ध का अर्थ की उत्पत्ति संविदा विधि के क्षेत्र प्रतिफल के अपवाद के रूप में हुई। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे की ओर कुछ छूट या लाभ देने का अवसर देता है और दूसरा ऐसे वचन के आधार पर अपनी स्थिति को बदल देता है तो वचन देने बालों को यह नहीं कहने दिया जायेगा कि उसका वचन बिना किसी प्रतिफल के था।
वचनात्मक विबन्ध का अर्थ का विशेष उदाहरण सेण्ट्रल लन्दन प्रापर्टी ट्रस्ट बनाम हाईट्रीज हाऊस लि. 1947 का वाद कई फ्लैट्स वाला एक भवन दस वर्ष के लिए किराये पर उठाया गया। लड़ाई छिड़ गयी। भवनखाली हो गया। किरायेदार पूरा किराया नहीं दे पा रहा था। मकान मालिक आधा किराया करने के लिए मान गया और लड़ाई के दौरान आधा किराया लेता रहा।
लड़ाई खत्म होते ही लोग शहरों की ओर लौट पड़े और सब मकान फिर से भर गये। मकान मालिक ने आगामी पूरा किराया माँगा। और पिछले साल का बाकी आधा किराया भी माँगा न्यायालय ने कहा कि वह आगे के लिए पूरा किराया माँग सकता था क्योंकि किराया घटाना और रद्द करने का हक वह रखता था।
उसने छूट दी और स्वयं उसी छूट के अनुसार आधा किराया लेता रहा। अब वह यह नहीं कह सकता था कि पिछले वर्ष के लिए भी उसे पूरा किराया मिलना चाहिए। इसलिए उसे यह कहने से विबन्धित कर दिया कि उसका केवल आधा किराया स्वीकार करने का करार बिना प्रतिफल के था।
विधर्व नैमियर इण्डस्ट्रीज लि. बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1994 बाम्बे के वाद में कहा कि एक सरकारी प्रस्ताव में यह बात आयी थी कि जो जंगल का ठेका दिया गया है वह तीस वर्ष के लिए होगा और प्रत्येक तीन वर्ष के बाद कीमतें संशोधित की जायेगी, सरकार ने इसे बदलकर प्रतिवर्ष करना चाहा, कोई विवन्ध नहीं।
शीतला प्रसाद दुबे बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1999 इलाहाबाद 1999 वाद में व्यक्ति जो किसी करार के माध्यम से लाइसेन्स पाने का लाभ लेता है, वह करार की शर्तों से बचने के प्रयास में सफल नहीं हो पायेगा। विबन्ध साम्या का नियम है। आधुनिक वर्षों में इस नियम ने नवीन आयाम प्राप्त किया है। इस देश में तथा इंग्लैंड में एक नवीन प्रकार का विवन्ध अर्थात् वचनीय विबन्ध न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कर पाया है।
वचनीय विबन्ध को कई नामों से जाना जाता है। जैसे-वचनीय विबन्ध, आवश्यक विवन्ध, अर्द्ध विबन्ध तथा नवीन विवन्ध अन्याय से बचने के लिए यह साम्या द्वारा उद्भव एक सिद्धान्त है और यद्यपि इसे वचनीय विवन्ध कहा गया है यह न तो संविदा और न ही विबन्ध के क्षेत्र में आता है। वचनीय विबन्ध का वास्तविक सिद्धान्त है।
न्यायालय यह साम्या के विरुद्ध मानता है कि प्रतिज्ञाकर्त्ता को उसकी प्रतिज्ञा से मुकरने की अनुमति दी जाये। भारत में वचनीय विबन्ध को न सिर्फ पूर्णरूप से अपना लिया गया है परन्तु जिस व्यक्ति को प्रतिज्ञा की गई है उसके लिए वाद कारण के रूप में मान्यता भी दी गई है। इस प्रकार की प्रतिज्ञाओं को लागू करने में प्रतिफल की आवश्यकता के मार्ग में खड़े रहने की अनुमति नहीं दी गयी है। वचनीय विवन्ध के सिद्धान्त को लागू करने से पूर्व यह साबित करना होगा कि
(1) कुछ भविष्य में करने के लिए कोई वचन व्यपदेशन किया गया था।
(2) उस व्यपदेशन के अनुरूप करने तथा उन पक्षकारों में मध्य वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने का आशय था तथा
(3) सह वचन या आश्वासन ऐसा था जिस पर दूसरी ओर के पक्षकार ने अपने हित के प्रतिकूल कार्य किया था। राज्य सरकार के विरुद्ध वचनीय विबन्धन के सिद्धान्त का लागू होना-वचनीय विबन्ध के सिद्धान्त को सरकार के विरुद्ध लागू किया गया है और प्रशासकीय आवश्यकता पर आधारित प्रतिवाद को साफ तौर पर इन्कार कर दिया गया है यदि सरकार यह जानते हुए कोई प्रतिज्ञा करती है कि जिस पर प्रतिज्ञाग्रहीता द्वारा कार्य किया जायेगा और वास्तव में प्रतिज्ञाग्रहीता उस पर विश्वास करते हुए अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता है।
इस दशा में सरकार को अपनी प्रतिज्ञा से बाध्य माना जायेगा और प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञाग्रहीता की पहल पर सरकार के विरुद्ध लागू किया जायेगा भले ही उस प्रतिज्ञा के लिए कोई प्रतिकूल नहीं है उस गणतंत्र में जो विधि के शासन से शासित हो कोई भी विधि के ऊपर नहीं है प्रत्येक व्यक्ति दूसरे की भाँति पूर्णरूप से विधि के अधीन है और सरकार उसका अपवाद नहीं है।
उदाहरण- इस नये प्रकार के विबंध को मोतीलाल पदमपत सुगर मिल्स बनाम यू.पी. राज्य, 1979 के प्रसिद्ध मुकदमें में उच्चतम न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति भगवती ने कहा-प्रत्यर्थी के दिनांक 23 जनवरी 1969 के पत्र से यह स्पष्ट था कि प्रत्यर्थी द्वारा
सरकार की ओर से स्पष्ट तौर पर एक प्रतिवेदन किया था और अपीलकर्ता वनस्पति कारखान की उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष तक उत्तर प्रदेश में बेची गई वनस्पति पर बिक्री कर से छूर प्राप्त होगी।
दिनांक 23 जनवरी, 1969 के पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्यर्थी ने सरकार के मुख्य सचिव की हैसियत से यह प्रतिवेदन किया था अतः यह सरकार की ओर से किया गय प्रतिवेदन होगा। अपीलकर्त्ता ने सरकार के इस प्रतिवेदन पर विश्वास करके कई संस्थाओं से ऋण लिया था तथा डी स्मिथ बम्बई से प्लाण्ट तथा मशीनरी भी क्रय कर ली थी और कानपुर में एक कारखाना लगाया अतः वचनीय विबन्ध के लिए आवश्यक सभी तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान थे।
तथा सरकार को प्रतिवेदन का पालन करने के लिए बाध्य किया जायेगा तथा अपीलकर्त्ता को उत्पादन की तिथि से तीन वर्ष तक उ.प्र. में बेची गयी वनस्पति पर बिक्री कर से छूट प्राप्त होगी। सरकार वचनीय विबन्धन के सिद्धान्त पर भरपाई के लिए बाध्य की जायेगी।
परन्तु बाद में न्यायालय ने आर. के. डेका बनाम भारत संघ, 1922 दिल्ली एव के. राम मोहन राव बनाम इन डाउमेंटस कमिश्नर इन कर्नाटक, बंगलौर एवं अन्य, कई मामलों में यह कहा कि अगर सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करती है या उसके द्वारा निर्धारित की गई नीति लोकहित के विरुद्ध है एवं वह ऐसी नीति बदल लेती है तो वचनात्मक विबंध का सिद्धान्त लागू नहीं होगा।
इसे भी पढ़ें…
- साइबर अपराध क्या है?
- साइबर कैफे किसे कहते हैं?
- बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर टिप्पणी
- वित्तीय अपराध पर संक्षिप्त लेख
- बाल अश्लीलता क्या है?
- साइबर अश्लीलता क्या है
- हैकिंग कैसे करते हैं?
- हैकिंग क्या है?
- अन्तर्राष्ट्रीय साइबर अपराध की विधि
- साइबर अपराध क्या है?






